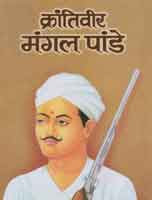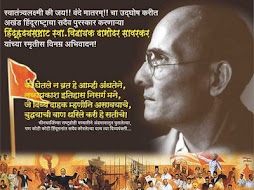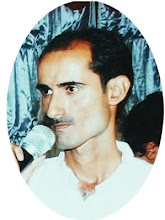सोमवार, 24 मई 2010
महंगाई ने लगाई चहुंओर आग
बढ़ती महंगाई और खाघान्न की समस्या से चहुंओर आग लगी हुई है। इस आग से सबसे प्रभावित है आम नागरिक जिसे दो वक्त की रोटी जुटाना भी अब भारी पड़ रहा है। हालांकि इस तथ्य को झुठलाया नहीं कहा जा सकता की बढ़ती महंगाई के नेपथ्य में सरकारी नीतियों के साथ-साथ संपूर्ण विश्व की गतिविधियां भी कहीं न कहीं कारक के रूप में उपस्थित रहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार सारे मामले को वैश्विक घटनाओं पर थोपकर अपना पल्ला झाड़ ले। विकास का पहिया निरंतर घूमता रहे इसके लिए मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता प्रथम अनिवार्य शर्त है, जिसकी अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। इस समस्या को दो विभिन्न आयामों से देखकर वैश्विक परिपेक्ष्य में सरकार की स्थिति को आंका जा सकता है। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने विश्व में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया था। इस क्रांति की बदौलत न केवल यूरोप विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, अपितु संपूर्ण विश्व ही उसके बनाए रोड मैप का अनुसरण कर प्रगति के पथ पर आगे बढऩे लगा। औद्योगिक क्रांति ने विकास की वो बुनियाद डाली जिस पर आज संपूर्ण संसार की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से टिकी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी औद्योगिक क्रांति की देन माने जा सकते हंै। औद्योगिकीकरण की रफ्तार बनाए रखने के लिए जब कच्चे माल तथा औद्योगिकीकरण के कारण फैक्ट्रियो में बने बहुतायात उत्पादों को खपाने के लिए बस्तियों की आवश्यकता पड़ी तब उपनिवेशवाद का एक नया दौर भी जन्मा था।यह कहना अतिश्योक्ति पूर्ण नहीं है कि औद्योगिकीकरण की वजह से ही हरित एवं श्वेत क्रांति भी अस्तित्व में आ सकीं। बहरहाल, 19वीं शताब्दी की समाप्ति तक वैश्विक मंच और विभिन्न देशों की भौगोलिक सीमाओं में अनेक परिवर्तन आए और वैश्वीकरण की भावना को बढ़ावा मिलने लगा। आ£थक क्षेत्र में सहयोग की बढ़ती आवश्यकता ने सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष:प से एक-दूसरे पर निर्भर बनाकर, स्वयं को सर्वेसर्वा मानने की भावना को रसातल में पहुंचा दिया। यही कारण है कि जब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका पर सबप्राइम संकट छाया तो भारत सहित अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उससे बचने के उपाय ढूंढे जाने शु: हुए। इसी प्रकार खाड़ी देशों से विभिन्न देशों में निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्ररोक्ष:प से प्रभावित करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का बढऩा, महंगाई के बढऩे की दिशा तय करता है, ऐसे में यह कह पाना काफी कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होने वाली हलचलों से कोई देश अब अछूता भी रह सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो महंगाई का मुद्दा एकमात्र सपं्रग सरकार को चिंता का कही विषय नहीं, अपितु इस प्राय: प्रत्येक देश की सरकार अपने-अपने स्तर पर जूझ रही है। वस्तुत: वैश्वीकरण के लाभ और हानि बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की तरह हो चुके हैं जिसके ज्यादा एक्सपोजर से हाय-हाय तो अदाओं पर वाह-वाह करने से लोग नहीं चूकते। कुछ समय पूर्व कैरेबियाई देशों में जो खाधान्न समस्या को लेकर घटनाएं घटित हुई वह इसी प्रभाव का परिणाम मानी जा सकती हैं। इसको लेकर विश्व भर के देश चिंतित होकर अनेक उपाय कर रहे है। आंकड़ों के मुताबिक गत् ढाई दशकों में विश्व का अनाज भंडारण अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच चुका है तथा खाद्यान्न की कीमतें रिकॉर्ड स्तर को पार कर रही हंै। इसको देखते हुए विश्व के कई देशों में अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जा रहे है। तो कहीं आयात पर से प्रतिबंध हटाएं जा रहें हैं। वस्तुत सारी स्थिति ही इस ओर इशारा कर रही हैं कि महंगाई का बढऩा एक मात्र सरकार की असफल नीतियों का परिणाम नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नही लगाया जा सकता कि खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को कम करने में सरकार द्वारा किसी पहल की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी खाद्यान्न की कमी और उनकी कीमतों में वृद्धि को सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखते हंै। चूंकि खाद्यान्न की कीमतों पर अंकुश नहीं लगता, तो इसका सीधा प्रभाव आ£थक विकास और अर्थव्यवस्था पर पडऩा तय है। लेकिन देश में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई इसे समझना भी आवश्यक है। महंगाई बढऩे के दो प्रमुख कारणों सब प्राइम संकट और बढ़ती तेल की कीमतों को निकाल दें तो इसके इत्तर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है जो देश में खाद्यान्न कीमतों की बढ़ोत्तरी के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है और इसका सबसे प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा है। कृषि क्षेत्र के प्रति बरती जाने वाली इसी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग अपने परंपरागत् खेती-बाड़ी के व्यवसाय को छोड़कर अन्य उद्यमों के प्रति आकृष्ट हुआ। चूंकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि ही है, परंतु उसके प्रति बरती गई सरकारी उपेक्षा किसानों का इस दिशा से मोहभंग करने में काफी रही। समय पर सरकारी ऋण न मिलने से परेशान किसान जहां गैर परंपरा गत् उद्यमों की ओर कूच करने लगे वहीं ऋण के बोझ तले दबे किसान एक के बाद एक आत्महत्या करने को बाधित हुई। पिछले कुछ वर्षों का दौर कौन भुला सकता है जब किसानों की आत्महत्या से संबंधित खबरों में समाचार पत्र और टी-वी- चैनल अटे पड़े थे। सहायता के नाम पर नाम मात्र सरकारी धनराशि से किसानों का कितना भला हुआ, यह सहज ही समझा जा सकता है। समय से पूर्व संभावित खाद्यान्न समस्याओं का आंकलन करने में सभी पुरोधा भयंकर चूक कर बैठे। अन्यथा यह कैसे संभव है कि सेंसेक्स की उड़ान पर विकास दर की भविष्यवाणी करने वाले बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप घटती फसल उत्पादकता पर मंथन नहीं कर सके। हां, इस संदर्भ में यह रियायत भले ही ली जा सकती है कि संपूर्ण विश्व में तमाम अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिकों के आंकड़ों से इत्तर यह स्थिति उत्पन्न हुई है।और इसका सबसे प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा है। कृषि क्षेत्र के प्रति बरती जाने वाली इसी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग अपने परंपरागत् खेती-बाड़ी के व्यवसाय को छोड़कर अन्य उद्यमों के प्रति आकृष्ट हुआ। चूंकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि ही है, परंतु उसके प्रति बरती गई सरकारी उपेक्षा किसानों का इस दिशा से मोहभंग करने में काफी रही। समय पर सरकारी ऋण न मिलने से परेशान किसान जहां गैर परंपरा गत् उद्यमों की ओर कूच करने लगे वहीं ऋण के बोझ तले दबे किसान एक के बाद एक आत्महत्या करने को बाधित हुई। पिछले कुछ वर्षों का दौर कौन भुला सकता है जब किसानों की आत्महत्या से संबंधित खबरों में समाचार पत्र और टी-वी- चैनल अटे पड़े थे। सहायता के नाम पर नाम मात्र सरकारी धनराशि से किसानों का कितना भला हुआ, यह सहज ही समझा जा सकता है। समय से पूर्व संभावित खाद्यान्न समस्याओं का आंकलन करने में सभी पुरोधा भयंकर चूक कर बैठे। अन्यथा यह कैसे संभव है कि सेंसेक्स की उड़ान पर विकास दर की भविष्यवाणी करने वाले बढ़ती जनसंख्या के अनरूप घटती फसल उत्पादकता पर मंथन नहीं कर सके। हां, इस संदर्भ में यह रियायत भले ही ली जा सकती है कि संपूर्ण विश्व में तमाम अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिकों के आंकड़ों से इत्तर यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जानकारों का मानना है कि देश में हरित क्रांति के उपरांत एक प्रकार से कृषि क्षेत्र की उपेक्षा प्रारंभ करनी शरू हो गई है। देश में लगातार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलता रहा, जबकि कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत सुविधाओं से जुझने के साथ-साथ अपने विस्तार के लिए तरसते रहें। जिसका परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या के अनुरूप औसतन वार्षिक पैदावार में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी।
आधुनिक विज्ञान ऋणी है देव संस्कृति का
क्रान्तियों के अविराम दौर को देखने और समझने वाले कल के महापरिवतर्न के बारे में विश्वस्त है । इस विश्वसनीयता ने सोच विचार में रुचि रखने वालों के मन में जिस जिज्ञासा को जन्म दिया है, वह है कल के जीवन की रूपरेखा उसका स्वरूप और संस्कृति । एक तरफ तर्कों और प्रयोगों की कसौटी पर तथ्यों को परखने वाला विज्ञान है । दूसरी ओर विश्वासों की बैसाखी पर टिका हुए विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों का समूह है । संवेदनशील हो सोचने वाले मानववादियों, दार्शनिक का अपना वर्ग है, उनकी अपनी चिन्तन प्रणालियाँ हैं । कल की जिन्दगी इनमें से किसे चुनेगी? अथवा किसमें वह सामर्थ्य है जो स्वयं को भावी-समाज के योग्य ठहरा सके । कुछ भी हो सवाल नवयुग की नयी संस्कृति की खोज का है । शुरुआत से खोज जीवन की मूलवृत्ति रही है । आवश्यकता आविष्कार की जननी है के सर्व प्रचलित सिद्धान्त ने समय-समय पर अनेकों उभार लिए हैं । आवश्यकता सभी को होती है-पशु हो या मनुष्य पर इनके स्वरूप में भेद हैं । पशुओं ने अपनी जिन्दगी की जरूरतों को पूरा करने स्वयं की वंश-वेलि को बचाए रखने के लिए कम खोजें नहीं की । प्राणिशास्त्र इसी के अध्ययन का इतिहास है । प्रकृति की सूक्ष्म हलचलों को पढऩे में सक्षम-चीटीं, कुत्ते, संगठन करने वाली दीमक, मधुमक्खी आदि के प्रयासें को देखकर दंग रहना पड़ता है । उनमें से अनेकों की अतीन्द्रिय सामर्थ्य का लोहा मानने के लिए सभी विवश हैं । पर इतने पर भी पशु भी किसी संस्कृति का निमार्ण नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं की प्रकृति और प्रवृति में परिवतर्न करने की न जरूरत महसूस की और न स्वयं में इसे कर सकने की सामर्थ्य का ही अनुभव किया । खोजी मनुष्य ने अपनी इसी विशेषता के कारण सभ्यताएँ निमिर्त की, संस्कृतियाँ रचीं और जीवन को अनूठा सौन्दर्य प्रदान किया । मनीषी स्टिच-स्टीफेन के ग्रन्थ रिसर्च एण्ड प्रोसेज के शब्दों में कहें तो इस विराट ब्रह्माण्ड में शक्ति-चेतनता की अनेकों धाराएँ अनेकों स्तर हैं । इनमें से प्रत्येक स्तर का अपना वैभव अपनी उपलब्धियाँ हैं, खोज का अर्थ इनमें से किसी स्तर से अपना गहरा सामजस्य बिठाना उसे मूर्त रूप देना है । प्रत्येक खोज का जन्म आवश्यकता से उत्पन्न इच्छा में होता है । इच्छा अपनी परिपक्व दशा में विचार और जिज्ञासा का रूप लेती है । जिज्ञासा के उपलब्धि की ओर बढ़ते कदम प्रक्रिया को जन्म देते हैं । प्रक्रिया की परिपूणर्ता में सपना साकार हो उठता है । समय के प्रवाह में मनुष्य की अंत: प्रकृति और ब्रह्म प्रकृति में अनेकों परिवतर्न घटित होते रहते हैं । संसार का स्वरूप भी अपने में व्यापक फेर-बदल करता रहता है । इन सारी उलट-फेर में फँसकर प्रक्रियाओं में परिवतर्न आना स्वाभाविक है । लेकिन उपलब्धि का सिलसिला वही रहता है । उदाहरण के लिए आग को ले, अग्नि तत्व सृष्टि के उदय काल से विद्यमान है । शुरूआत के दिनों इसकी जरूरत पडऩे पर मानव ने पत्थर रगड़कर इसे हासिल किया । तब से आज तक अग्नि उत्पादक प्रक्रियाओं में भारी अन्तर आ चुका है पर अग्नि वही है । नृतत्व विज्ञानियों के अनुसार आज से हजारों साल पहले भी आदमी ने अपनी सभ्यता के गौरवपूर्ण शिखरों को छुआ है । जिन्दगी के व्यापक दायरे के हर बिन्दु पर उसने तरह-तरह के शोध अध्ययन किए । समग्र जीवन पद्धति को रचने वाली संस्कृति के निमार्ण में सफल हुआ । महायोगी अनिवार्ण के ग्रन्थ वेद मीमांसा के अनुसार उसने अन्त: और प्रकृति पर अनूठे प्रयोग किए । ऐसे प्रयोग जिनसे मनुष्य देवता बन गया और धरती स्वर्ग । समय के थपेड़ों और नई पीढ़ी की उत्तरदायित्वहीनता के कारण ढेर की ढेर प्रक्रियाएँ खो गई । उन प्रक्रियाएँ के खोने का परिणाम है कि मनुष्य आज न जाने कितनी उपलब्धियों से वंचित है? वतर्मान परिस्थियाँ इतनी बदली हुई है कि वेदों के आख्यान- पुराणों के विवरण, शास्रों के वचन सुनने वालों को नानी की कहानी मालूम पड़ते हैं, जब कभी कोई ऋषि दयानन्द परमहंस विशुद्धानन्द, उन तथ्यों को अपने जीवन में प्रमाणिक कर लोक-जीवन को झकझोरता है सभी थोड़े समय उसे कौतुक और अतिमानव का सम्मान दें अपने लिए असम्भव बता किसी गहरी नींद खोने लगते हैं । इस असम्भव और आश्चयर्जनक के पीछे झाँकने वाले तथ्यों को परखे तो प्रक्रियाओं का मौलिक अन्तर समझ पड़ता है । प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ डा. गोपीनाथ कविराज के अध्ययन भारतीय संस्कृति साधना शब्दों में आज की शोध प्रक्रियाएँ जिन्हें विज्ञान की विभिन्न शाखा-उपशाखाओं का समूह कहले विश्लेषण करने में समर्थ बुद्धि की उपज है । देव संस्कृति के विभिन्न पक्षों की खोज के पीछे अन्तज्ञार्न सम्पन्न संवेदनशील मन को ढूँढ़ा जा सकता है । आज के जीवन में यदा-कदा ऐसे अवसर आ जाते हैं, जब पुरानी शोध को नवीन मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है । परिणति आश्चयर्जनक ढंग से सुखद होती है । लेकिन पुरानी प्रक्रियाओं के खो जाने से आधुनिक प्रयोगकर्ताओं को इस विवशता का सामना करना पड़ता है कि ऋषि मुनि कहे जाने वाले शोध विज्ञानी यन्त्रों और बहुमूल्य प्रयोगशालाओं के अभाव में इन निष्कर्षों तक कैसे पहुँच सकें, समस्या का सुलझा सकने में अक्षम बुद्धि को एक ही बात समझ मे आती है कि इन सब तथ्यों को संयोग कहकर चुप्पी साध लें । पर संयोग एक-आध हो सकते हैं । मानवीय ज्ञान के विविध क्षेत्रों में इनका भरा-पूरा सिलसिला इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं तथ्यांकन की कोई पुनमूर्ल्यांकन के अपने मौलिक अधिकार के लिए गुहार लगा रही है । चरक का आयुविर्ज्ञान, वराहमिहिर, आयर्भट्ट की खगोल गणनाएँ, पतंजलि का मानसशास्र, गोरक्षनाथ की हठयोग प्रणाली, विभिन्न दाशर्निक पद्धतियों के सृष्टि और मनुष्य सम्बन्धी गहरे सवेर्क्षण प्रयोगों की कसौटी पर कसने पर यह मानने के लिए विवश करते हैं कि यह सब कल्पना लोक की उड़ाने नहीं हैं । तब क्या इन सबके पास आज सी सुसज्जित प्रयोगशालाएँ थी जिनकी न तो उल्लेख मिलता है न अवशेष? इस प्रश्न का सुसंगत उत्तर इतना ही है कि प्रयोगों की प्रणाली तो थी पर आज से भिन्न । उन दिनों प्रारम्भ से ही अन्त: प्रकृति को तरह-तरह के गम्भीर प्रयोगों द्वारा इस लायक बना दिया जाता था कि वह सृष्टि के विभिन्न रचनाक्रमों और इसकी उपादेयता को सम्यक् ज्ञान अजिर्त कर सकें । ऐसे शोधार्थी के रूप में चरक और उनके सहयोगी किसी पौधे के प्राण स्पंदनों से अपने अन्तर्बोध सम्पन्न मन का एकाकार करके-पौधे की गुणवत्ता, उसके भाग विशेष की रोगनिवारण की विभिन्न क्षमताओं का ज्ञान अजिर्त कर लेते थे । परीक्षणों का व्यापक सिलसिला प्रयोगों की गुणवत्ता को शत-प्रतिशत ठीक ठहराता था । यही कारण है कि आयुवेर्द के प्राचीन ग्रन्थों में पौधों के गुण-स्वभाव उनके विभिन्न भागों की रोगनिवारण सामर्थ्य-प्रयोग विधि का ब्योरेवार विवरण तो मिलता है, पर पौधे के रासासनिक संगठन और सूक्ष्म विश्लेषण का अभाव है । यही बात ज्ञान की अन्य धाराओं के सन्दर्भ में है । प्राचीन ज्ञान की प्राय: सभी शाखाओं-उपशाखाओं की उपलब्धि में प्रक्रिया का यही स्वरूप दिखाई देता है । इसका एक ही कारण है इसकी सवर्तोजयी प्रामाणिकता प्राचीन शास्रों में ज्ञान की चार विधियों का उल्लेख मिलता है । इन्द्रियानुभूति द्वारा अन्तबोर्ध सम्पन्न मन से, विश्लेषण क्षमता सम्पन्न बुद्धि से और गहरे आत्मिक तादात्म्य द्वारा । आधुनिक समय में ऋषि अरविन्द लाइफ डिवाइन में इसी अन्तिम विधि को श्रेष्ठ बताया है । देव संस्कृति को जन्म देने वाले इस विधि में निष्णात् थे । यही कारण है उन्होंने इस उत्कृष्ट विधि के रहते निम्न विधियों का कम ही प्रयोग किया है ।
संस्कृति की केन्द्रिय धुरी नारी शक्ति
भारतीय संस्कृति का प्रधान केन्द्रीय तत्व है-भाव-संवेदना । इस गुण की प्रचुरता जिसमें है, वह नारी शक्ति देव संस्कृति के विकासक्रम में एक धुरी की भूमिका निभाती आयी है । ऋषिगण आदि सत्ता महामाया, जिसके आधार पर सृष्टि की संरचना संभव हुई है, को विधाता भी कहते आये हैं व माता भी । प्राणियों का अस्तित्व ही यदि इस धरती पर है तो उसके मूल में मातृशक्ति की प्राणियों पर अनुकम्पा है । सृजन शक्ति के रूप में इस संसार में जो कुछ भी सशक्त सम्पन्न, विज्ञ और सुन्दर है, उसकी उत्पत्ति में नारी तत्व की ही अहम् भूमिका है । देवसंस्कृति में सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में विज्ञान प्रधान और गायत्री-सावित्री के रूप में ज्ञानप्रधान चेतना के बहुमुखीय पक्षों का विवेचन अनादि काल से होता आया है । परम पूज्य गुरुदेव ने नारी शक्ति के माध्यम से ही इक्कीसवीं सदी के आगमन की बात कही व घोषणा की है कि विश्व मानवता का भावी निर्धारण उन्हीं गुणों के आधार पर होने जा रहा है, जो आदि स्रजेता के रूप में नारीसत्ता के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं । पूज्य गुरुदेव ने लिखा है-देवत्त के प्रतीकों में प्रथम स्थान नारी का और दूसरा नर का है । लक्ष्मी-नारायण, उमा-महेश शची-पुरन्दर, सीता-राम, राधे-श्याम जैसे देव युग्मों में प्रथम नारी का और पश्चात् नर का उल्लेख होता है । वह मानुषी दीख पड़ते हुए भी वस्तुत: देवी है । श्रेष्ठ व वरिष्ठ उसी को मानना चाहिए । भाव संवेदना, धर्मधारणा और सेवा साधना के रूप में उसी की वरिष्ठता को चरितार्थ होते देखा जाता है ।ज्ज् वैदिक मान्याताओं के अनुसार नारी बिना, शक्ति के बिना यह सम्पूर्ण विश्व सार-शून्य है । सृष्टि विस्तार की दृष्टि से भी निस्संदेह पुरुष की अपेक्षा नारी की महत्ता अधिक है । वह पुरुषों की जननी है । उसकी सब कामना करें व उसके द्वारा पालित हों, ऐसा र्निदेश वैदिक ऋषि देते आये हैं । च्कन्याज् शब्द का अर्थ होता है सबके द्वारा वांछनीय सब उसकी कामना करें । ऐतरेयोपनिषद में स्पष्ट आता है- नारी हमारा पालन करती है, अत: उसकी पालन करना हमारा र्कत्तव्य है! अथर्ववेद में उसे सत्याचरण की अर्थात् धर्म की प्रतीक कहा गया है (सत्येनोत्रभित भूमि:) कोई भी धार्मिक कार्य उसके बिना अधूरा माना जाता रहा है । ऋग्वेद का ऋषि लिखता है-
च्ज्शुचिभ्राजा उषसो नवेद, यशस्वतीरपस्युवो नसत्या: ।ज्ज् (ऋग् 1/79/1)
अर्थात्-श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सेवा, समानता का प्रतीक नारी पवित्र, निष्कलंक, आचार के प्रकाश से सुशोभित, प्रात:काल के समान हृदय को पवित्र करने वाली, लौकिक कुटिलताओं से अनभिज्ञ, निष्पाप, उत्तमयश युक्त, नित्य उत्तम कर्म करने की इच्छा करने वाली, सकर्मण्य और सत्य व्यवहार करने वाली देवी है । एक भ्रान्तिपूर्ण मान्यता, कि कन्या का जन्म अमंगलकारी है, हमारी देश में मध्यकाल में पनपी व इसी कारण आधीजन शक्ति दोयमर्दजे की मानी जाने लगी । नारीशक्ति की अवमानना, तिरस्कार, होने लगा, जबकि संस्कृति के स्वर आदि काल से कुछ और ही कहते आए हैं । ऋग्वेद (6/75/5) में कहा गया है कि च्ज्वह पुरुष धन्य है, जिसके कई पुत्रियाँ हों तथा पुत्र से पिता को आनंद मिलता है, वहीं पुत्री से माता को बल्कि उससे भी अधिक (3/31-1-2) । उपनिषदों में भी यही बात स्पष्टत: सामने आई है । बृहदारण्यकेपनिषद् में विदुषी और आयुष्मती पुत्री पाने के लिए घी और तेल में चावल पकाकर खाने की विधि कही गयी है (6/4.17) । मनुस्मृति (9/13)में कहा गया है कि पुत्री को पुत्र के समान समझना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार आत्मा पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वह पुत्री के रूप में भी जन्म लेती है । महाभारत में सन्यास लेने की पात्रता उसी गृहस्थ को प्राप्त है, जिसने गृहस्थधर्म का पालन करते हुए सभी र्कत्तव्यों को पूरा कर लिया है । इन र्कत्तव्यों में अपनी पुत्रियों का विवाह कर देना प्रमुख है (महाभारत उद्योगपर्व 36-39) । मनुस्मृति में पिता के उत्तराधिकार को जो भाग पुत्री को देने का विधान है, उसका हेतु ध्यान देने योग्य है ।ज्ज् विवाह की चिन्ता और सार्मथ्य से बाहर दहेज के कारण लोकगीत मध्य काल में ऐसे रचे जाने लगे कि पुत्री जन्म ही अशुभ माना जाने लगा पंचतंत्र के कुछ आख्यानों में भी यह बात आयी । कालान्तर में मध्यकाल में यह यह धारणा खूब फली-फूली व स्त्रीधन की उपेक्षा शास्त्र वचनों की दुहाई देकर अधिक से अधिक की जाने लग । वस्तुत: यह कालक्रम के अनुसार पैदा हुई विकृति है । नहीं तो पिता के वात्सल्य का आदर्श तो हर युग की एक मान्य आस्था रही है । इसी आस्था के कारण रामायण में जनक कहते हें । च्ज्जिस सीता को मैं प्राणों से बढ़कर चाहता हूँ, उसे राम को सौंपकर मेरी वीर्यशुल्क की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगीज्ज् (वा.रा.बालकाण्ड 67/23) । यह भारतीय संस्कृति की ही चिर पुरातन मान्यता है कि जैसे पुत्र अपने पिता, पितामह इत्यादि पितरों को नरकों से तारता है, इसी प्रकार दौहित्र अपने नाना को । महाभारतकाल में एक चक्रनगर का निर्धन, विचारशील ब्राह्मण बकासुर की भेंट चढ़ाए जाने से अपनी कन्या को रोकता है व स्वयं जाने को तत्पर हो जाता है, तब भीम उसके स्थान पर जाते हैं । कुन्ती को पुत्री रूप में शूरसेन तथा किन्तुभोज ने पुत्र से अधिक प्यार देकर स्नेहपूर्वक पाला था । महर्षि कण्व शकुन्तला को दुष्यन्त के पास विदाई हेतु भेजते समय भावार्द्र हो उठते हैं वे कहते हैं, तो फिर कन्या बिछोह सामान्य गृहस्थों के लिए कितना असह्य होगा? (शाकुन्तल 2/6) इसेस समाज की सही अवस्था का परिचय मिलता है
च्ज्शुचिभ्राजा उषसो नवेद, यशस्वतीरपस्युवो नसत्या: ।ज्ज् (ऋग् 1/79/1)
अर्थात्-श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सेवा, समानता का प्रतीक नारी पवित्र, निष्कलंक, आचार के प्रकाश से सुशोभित, प्रात:काल के समान हृदय को पवित्र करने वाली, लौकिक कुटिलताओं से अनभिज्ञ, निष्पाप, उत्तमयश युक्त, नित्य उत्तम कर्म करने की इच्छा करने वाली, सकर्मण्य और सत्य व्यवहार करने वाली देवी है । एक भ्रान्तिपूर्ण मान्यता, कि कन्या का जन्म अमंगलकारी है, हमारी देश में मध्यकाल में पनपी व इसी कारण आधीजन शक्ति दोयमर्दजे की मानी जाने लगी । नारीशक्ति की अवमानना, तिरस्कार, होने लगा, जबकि संस्कृति के स्वर आदि काल से कुछ और ही कहते आए हैं । ऋग्वेद (6/75/5) में कहा गया है कि च्ज्वह पुरुष धन्य है, जिसके कई पुत्रियाँ हों तथा पुत्र से पिता को आनंद मिलता है, वहीं पुत्री से माता को बल्कि उससे भी अधिक (3/31-1-2) । उपनिषदों में भी यही बात स्पष्टत: सामने आई है । बृहदारण्यकेपनिषद् में विदुषी और आयुष्मती पुत्री पाने के लिए घी और तेल में चावल पकाकर खाने की विधि कही गयी है (6/4.17) । मनुस्मृति (9/13)में कहा गया है कि पुत्री को पुत्र के समान समझना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार आत्मा पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वह पुत्री के रूप में भी जन्म लेती है । महाभारत में सन्यास लेने की पात्रता उसी गृहस्थ को प्राप्त है, जिसने गृहस्थधर्म का पालन करते हुए सभी र्कत्तव्यों को पूरा कर लिया है । इन र्कत्तव्यों में अपनी पुत्रियों का विवाह कर देना प्रमुख है (महाभारत उद्योगपर्व 36-39) । मनुस्मृति में पिता के उत्तराधिकार को जो भाग पुत्री को देने का विधान है, उसका हेतु ध्यान देने योग्य है ।ज्ज् विवाह की चिन्ता और सार्मथ्य से बाहर दहेज के कारण लोकगीत मध्य काल में ऐसे रचे जाने लगे कि पुत्री जन्म ही अशुभ माना जाने लगा पंचतंत्र के कुछ आख्यानों में भी यह बात आयी । कालान्तर में मध्यकाल में यह यह धारणा खूब फली-फूली व स्त्रीधन की उपेक्षा शास्त्र वचनों की दुहाई देकर अधिक से अधिक की जाने लग । वस्तुत: यह कालक्रम के अनुसार पैदा हुई विकृति है । नहीं तो पिता के वात्सल्य का आदर्श तो हर युग की एक मान्य आस्था रही है । इसी आस्था के कारण रामायण में जनक कहते हें । च्ज्जिस सीता को मैं प्राणों से बढ़कर चाहता हूँ, उसे राम को सौंपकर मेरी वीर्यशुल्क की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगीज्ज् (वा.रा.बालकाण्ड 67/23) । यह भारतीय संस्कृति की ही चिर पुरातन मान्यता है कि जैसे पुत्र अपने पिता, पितामह इत्यादि पितरों को नरकों से तारता है, इसी प्रकार दौहित्र अपने नाना को । महाभारतकाल में एक चक्रनगर का निर्धन, विचारशील ब्राह्मण बकासुर की भेंट चढ़ाए जाने से अपनी कन्या को रोकता है व स्वयं जाने को तत्पर हो जाता है, तब भीम उसके स्थान पर जाते हैं । कुन्ती को पुत्री रूप में शूरसेन तथा किन्तुभोज ने पुत्र से अधिक प्यार देकर स्नेहपूर्वक पाला था । महर्षि कण्व शकुन्तला को दुष्यन्त के पास विदाई हेतु भेजते समय भावार्द्र हो उठते हैं वे कहते हैं, तो फिर कन्या बिछोह सामान्य गृहस्थों के लिए कितना असह्य होगा? (शाकुन्तल 2/6) इसेस समाज की सही अवस्था का परिचय मिलता है
गाथा इस देश की गायी विदेशीयों ने
भारतवर्ष की शक्ति और समृद्धि ज्ञान और गुरुत्व विश्वविख्यात है । प्राचीन काल की श्रेष्ठतम उपलब्धियों से भरपूर साहित्य और इतिहास हमें प्रतिक्षण उस गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है । पूर्वजों की आत्माओं का प्रकाश अब इस देश के कण-कण को जागृति का संदेश दे रहा है । यह बात हर एक नागरिक के हृदय में समाई हुई है, वह आत्माभिमान अभी तक मरा नहीं । किन्तु काल के दूषित प्रभाव के कारण आज आर्य जाति सब तरह से दीन-हीन बन चुकी है । अब उसका कदम केवल विनाश की ओर ही बढ़ रहा है । जानते हुए भी हम अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को भुलाये बैठै हैं । हमारी गाथायें विदेशों में बिक गई । हमारे ज्ञान की एक छोटी सी किरण पाकर पाश्चात्य देश अभिमान से सिर उठाये खड़े हैं और हम अपने पूर्वजों की शान को भी मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं । कठोर बनने का कोई उद्देश्य नहीं है । कटु बात कहकर अपने ही आत्मा के कणों का जी दुखाना नहीं चाहते किन्तु जो दुर्गति हमारी संस्कृति की इन दिनों हो रही है, उसे देखकर हृदय में सौ-सौ बरछों का-सा प्रहार लग रहा है । आत्मा की इस आवाज को कोई धर्मभिमानी, राष्ट्र हितैषी तथा जाति के गौरव के लिये प्राण अर्पण करने वाला ही समझ सकता है । आर्य संस्कृति का या हिन्दू धर्म का नाम उल्लेख करने में साम्प्रदायिक संकीर्णता का भाव नहीं आना चाहिए । हमारी संस्कृति दिव्य-संस्कृति है । उसमें प्राणिमात्र के हित की व्यवस्था है । यह उद्बोधन केवल इसलिये है कि उस चिर-सत्य का प्रादुर्भाव केवल इसी भूमि में हुआ है, इसी से हम उसे एक विशेष सम्बोधन से विभूषित करते हैं, अन्यथा हिन्दू-धर्म को क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व है । काउन्ट जोन्स जेनी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया है- भारतवर्ष केवल हिन्दू धर्म का ही घर नहीं है वरन् वह संसार की सभ्यता का आदि भण्डार है ।ज्ज् संसार में भारतवर्ष के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति के कारण हैं । यह शब्द प्रो.लुई रिनाड ने व्यक्त किये है । इन शब्दों से भी यही तथ्य प्रकाशित होता है कि भारत समग्र विश्व का है और सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रेमपाश में आबद्ध है । अनादि काल से धर्म की, संस्कृति और मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है । धरती की अनुपम कृति यह देश भला किसे प्यारा ने होगा? भारतवर्ष ने जो आध्यात्मिक विचार इस संसार में प्रसारित किये हैं । वे युग-युगान्तरों तक अक्षुण्ण रहने वाले हैं । उनसे अनेक सुषुप्त आत्माओं को अनन्त काल तक प्रकाश मिलता रहेगा । भारतीय संस्कृति के प्रवाह का उद्गम वे चिन्तन शाश्वत और सनातन सत्य रहे है, जिनकी अनुभूति ऋषियों ने प्रबल तपश्चर्याओं के द्वारा अर्जित की थी, वह प्रवाह धूमिल भले ही हो गया हो किन्तु अभी तक भी लुप्त नहीं हुआ है । धार्मिक आध्यात्मिक एवं नैतिक क्षेत्र में ही हम सर्वसम्पन्न नहीं रहे वरन् कोई ऐसा नहीं छूटा जहाँ हमारी पहुँच न रही हो । आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक, व्यावहारिक तथा अन्य विद्याओं के ज्ञान-विज्ञान में भी हम अग्रणी रहे हैं । अपनी एक शोध में डा. थीवों ने लिखा है च्ज्संसार, रेखागणित के लिये भारत का ऋणी है यूनान का नहीं ।' प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रो. बेबर का कथन है-'अरब में ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से हुआ 'कोलब्रुक ने बताया है कि कोई अन्य देश नहीं, चीन और अरब को अकंगणित का पाठ पढ़ाने वाला देश भारतवर्ष ही है ।'यूनान के प्राचीन इतिहास का दावा है कि 'भारत के निवासी, यूनान में आकर बसे । वे बड़े बुद्धिमान, विद्वान और कला-कुशल थे । उन्होंने विद्या और वैद्यक का खूब प्रचार किया । यहाँ के निवासियों को सभ्य बनाया ।ज्ज् निसंदेह इतना सारा ज्ञान अगाध श्रम, शोध और लगन के द्वारा पैदा किया गया होगा । तब के पुरुष आलस्य, अरुचि, आसक्ति, अहंकार आदि से दूर रहें होंगे तभी तो वह तन्यता बन पाई होगी, जिसके बूते पर इतनी सारी खोज की जा सकी होगी । दुर्भाग्य की बात है कि आज वही भारतवर्ष विदेशियों के अनुकरण को ही अपनी शान समझता है । इस कार्य में जो जितना अधिक निपुण है, उसे उतनी ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है । विश्व के विविध विषयों के जब आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं तो देखकर तीव्र वेदना होती है कि उनमें भारतवर्ष पिछड़ी श्रेणी में आता है । शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे कमजोर, भारतीय की औसत आय संसार में सबसे कम, आरोग्य के नाम पर सबसे दु:खी दुर्बल और रोगग्रस्त, आहार में सबसे कम कैलोरी वाला, निर्धनता में सबसे पहले दर्जे का । अवनति की कोई हद नहीं । कोई क्षेत्र नहीं छूटा जहाँ मात न खाई हो । क्या वह समृद्धि हम फिर से देख सकेंगे, जिसका वर्णन प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एरियन ने इस तरह किया है- च्ज्जो लोग भारत से आकर यहाँ बसे थे वे कैसे थे? वे देवताओं के वंशज थे, उनके पास विपुल सोना था । वे रेशम के कामदार ऊनी दुशाले ओड़ते थे । हाथी दाँत की वस्तुयें व्यवहार में लाते थे और बहुमूज्य रत्नों के हार पहनते थे ।ज्ज् जो विध्वंसक विज्ञान और एटमी हथियार इन दिनों बन रहे हैं, उनसे भी बड़ी शक्ति वाले आयुध यहाँ वैदिक युग में प्रयुक्त हुये हैं । सरस्वती की उपासना के साथ-साथ शक्ति की भी समवेत उपासना इस देशें में हुई है । अथर्ववेद में उनके स्थानों पर जो च्ज्अशनिज्ज् शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ आजकल की भीमकाय तेपों जैसा ही है प्रोफेसर विल्सन का कथन है-ज्ज्गोलों का अविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था । योरोप के सम्पर्क में आने के बहुत समय पहले उनका प्रयोग भारत में होता था ।ज्ज् कर्नल रशब्रुक विलियम ने एक स्थान पर लिखा है-ज्ज्शीशे की गोलियाँ और बन्दूकों के प्रयोग का हाल विस्तार से यर्जुवेद में मिलता है । भारतवर्ष में तोपों और बन्दूकों का प्रयोग वैदिक काल से ही होता था ।
सृष्टि का प्रथम मानव आर्यार्वत्त में जन्मा
छान्दोग्योपनिषद में एक कथा आती है । इन्द्र तथा विरोचन दोनों ज्ञान प्राप्ति के लिए स्रष्टा के पास गए । दोनों आत्मतत्व जानना चाहते थे । ब्रह्माजी ने कहा दोनों सज-धजकर अपना प्रतिबिम्ब जल में देखो । जो जल में दिखाई पड़े, वही आत्मा है । विरोचन संतुष्ट होकर लौट आए । उसने शरीर को सजाधजा व अपनी मुखाकृति देखी उसी से उन्हें संतोष मिल गया । किन्तु इन्द्र ने बारम्बार मनन किया-आत्म चिन्तन किया । पुन: बार-बार लौटकर प्रजापिता ब्रह्मा से प्रश्न किया । उन्हें समाधान मिला कि शरीर नहीं, यह स्थूल काया नहीं, वरन् आत्मसत्ता ही परमसत्य है । सजाना-सँवारना उसे चाहिए । उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई । विरोचन ने लौटकर दैहात्मवाद का प्रचार किया । उनने प्रतिपादन किया कि देह ही आत्मा है । इसी की सेवा-श्रृंगार साधना की जानी चाहिए । मरने पर शरीर को सुरक्षित, सुसज्जित किया जाना चाहिए । प्रलय तक आत्मा उसी में रहती है । जब अंतत: सृष्टि प्रलय के समय उसी नष्ट होगी तब कर्मों का निर्णय होगा, जबकि इन्द्र ने आत्मसत्ता के उत्कर्ष का प्रतिपादन किया व इसके लिए मानवधर्म का निर्धारण किया । साधना पद्धतियाँ बनीं जिसमें भोगों से त्याग की प्रधानता थी । यह कथा कितनी सत्य है, यह ज्ञात नहीं पर इस अलंकारिक प्रतिपादन से एक सत्य उभरकर आता है कि दो प्रकार की जातियाँ उपनिषद्कालीन समाज में थी एक आर्य जिसके प्रतिनिधि थे इन्द्र देवसत्ताओं के प्रतिनिधि, संस्कारी पुरुष । दूसरी दस्यु जातियाँ अथवा आनार्य जातियाँ । इन्हीं को सुर व असुर कहा गया । सुर वे जिनने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया तथा असुर वे जिनने धर्मधारणा के प्रति प्रमाद था देहसुख जिन्हें अधिक प्रिय था । विरोचन इन्हीं सत्तओं का प्रतीक है व इन्हें देहात्मवाद के संस्कारों के साथ आर्यार्वत्त से बहिष्कृत कर दिया गया । इनने ही शवों को च्ममीज् की तरह सुरक्षित रखने का प्रावधान बनाया, जिसमें राजा-प्रजा सभी को एक साथ सजा-धजा कर दफना दिया जाता था । यह कथा मनोरंजन हेतु नहीं, आदि संस्कृति भारतीय संस्कृति के विकास के विभिन्न आयामों को समझाने हेतु प्रस्तुत की गयी है । वस्तुत: प्रथम मानव इस क्षेत्र में भारतवर्ष में जन्मा व प्रचलित पाश्चात्य विकासवाद के विरुद्ध वह आदिम जाति का नहीं, अनगढ़ नरमानुष नहीं अपितु एक श्रेष्ठ मनुष्य था, सभ्य था, पूर्णत: संयमशील था तथा ज्ञानवान था, उसी से समग्र मानव जाति की उत्पत्ति व विकास का क्रम चला । महाभारत ही एक आख्या के अनुसार -
अभगच्छत राजेन्द्र देविकां विश्रुताम् । प्रसूर्तित्र विप्राणां श्रूयते भरतर्षभ॥
अर्थात्-सप्तचरुतीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई । प्रमाण यही बताते हैं कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति भारत के उत्तराखण्ड अर्थात् इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ही हुई ।
संसार भर में गोरे, पीले, लाल और श्याम (काले) ये चार रंगो के लोग विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं । एक भारत ही ऐसा देश है, जहाँ, इन चार रंगो का भरपूर मिश्रण एक साथ देखने को मिलता है । वस्तुत: श्वेत-काकेशस, पीले-मंगोलियन, काले-नीग्रो तथा लाल रेड इंडियन इन चार प्रकार के रंगविभाजनों के बाद वाँचवी मूल एवं पुख्य नस्ल है, जो भारतीय कहलाती है । इस जाति में उर्पयुक्त चारों का सम्मिश्रण है । ऐसा कहीं सिद्ध नहीं होता कि भारतीय मानव जाति उर्पयुक्त चारों जातियों की वर्ण संकरता से उत्पन्न हुई । उलटे नृतत्व विज्ञानी यह कहते हैं कि भारतीय सम्मिश्रण वर्ण ही यहाँ से विस्तरित होकर दीर्घकाल में जलवायु आदि के भेद से चार मुख्य रूप लेता चला गया । न केवल रंग यहाँ चारों के सम्मिश्रण पाए जाते हैं, वरन् भारतीयों का शारीरिक गठन भी एक विलक्षणता लिए है । ऊँची दबी, गोल-लम्बी मस्तकाकृति उठी या चपटी नाक लम्बी-ठगनी, पतली मोटी शरीराकृत, एक्जों व एण्डोमॉर्फिक (एकहरी या दुहरी गठन वाली) आकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं । यहाँ से अन्यत्र बस जाने पर इनके जो गुण सूत्र उस जलवायु में प्रभावी रहे, वे काकेशस, मंगोलियन, नीग्रॉइड व रेडइंडियन्स के रूप में विकसित होते चले गए । अत: मूल आर्य जाति की उत्पत्ति स्थली भारत ही है, बाहर कहीं नहीं, यह स्पष्ट तथ्य एक हाथ लगता है । पाश्चात्य विद्वानों ने एक प्रचार किया कि आर्य भारत से कहीं बाहर विदेश से आकर यहाँ बसे थे । संभवत: इसके साथ दूसरी निम्न जातियों को जनजाति-आदिवासी वर्ग का बताकर, वे उन्हें उच्च वर्ग के विरुद्ध उभारना चाहते थे । द्रविड़ तथा कोल, ये जो दो जातियाँ भारत में बाहर से आईं बतायी जाती हैं, वस्तुत: आर्य जाति से ही उत्पन्न हुई थीं, इनकी एक शाखा जो बाहर गयी थी पुन: भारत वापस आकर यहाँ बस गयी । भारतीय जातियों पर शोध करने वाले नतृत्व विज्ञानी श्रीनैफील्ड लिखते हैं कि भारत में बाहर से आए आर्य विजेता और मूल आदिम मानव (अरबोरिजिन) जैसे कोई विभाजन नही है । ये विभाग सर्वथा आधुनिक हैं । यहाँ तो समस्त भारतीयों में एक विलक्षण स्तर की एकता है । ब्राह्मणों से लेकर सड़क साफ करने वाले भंगियों तक की आकृति और रक्त समान हैं ।
मनुसंहिता(1(/43-44)का एक उदाहरण है
शनकैस्तु क्रियालोपदिना: क्षत्रिय जातय: । वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च॥
पौण्ड्रकाशचौण्ड्रद्रविडा: काम्बोजा: भवना: शका: । पारदा: पहल्वाश्चीना: किरता: दरदा: खशा:॥
अर्थात् ब्राह्मणत्व की उपलब्धि को प्राप्त न होने के कारण उस क्रिया का लोप होने से पोण्ड्र, चौण्ड्र, द्रविड़ काम्बोज, भवन, शक पारद, पहल्व, चीनी किरात, दरद व खश ये क्षत्रिय जातियाँ धीरे-धीरे शूद्रत्व को प्राप्त हो गयीं । स्मरण रहे यहाँ ब्राह्मणत्व से तात्पर्य है श्रेष्ठ चिन्तन, ज्ञान का उपार्जन व श्रेष्ठ कर्म तथा शूद्रत्व से अर्थ है निकृष्ट चिंतन व निकृष्ट कर्म । क्षत्रिय वे जो पुरुषार्थी थे व बाहुबल से क्षेत्रों की विजय करके राज्य स्थापना हेतु बाहर जाते रहे । मूल आर्य जाति ने उत्तराखण्ड से नीचे की भूमि में वनों को काटकर, जलाकर उन्हें रहने योग्य बनाया । वहाँ नगर बसाये । इससे पूर्व वहाँ कोई निवास नहीं करता था । इस प्रकार मूल निवासी के रूप में एक ही उत्पत्ति आर्यों के रूप में हिमालय के उत्तराखण्ड क्षेत्र में हुई । वहीं से मनुष्य जाति का सारे विश्व में विस्तार हुआ । आदि मानव हिन्दू समाज था । इस प्रकार शेष सभी धर्म-मत-जातियाँ-रेस-वर्ण कालान्तर में समय प्रवाह के साथ विकसित होते चले गए भारतीय आर्षग्रन्थ ऋग्वेद केवल भारतीय आर्यों की ही नहीं बल्कि विश्वभर के आर्यों (श्रेष्ठ मानवों) की सबसे प्राचीन पुस्तक है । मनुसंहिता यही बात कहती है-
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानव:॥
किन्तु भारत से बाहर जाने के बावजूद अपने धर्म आचरण के प्रति अनुराग के उनने अपने सम्बन्ध भारतवर्ष से बनाए रखे । महाभारत काल तक भारतीय नरेशों से उनके वैवाहिक सम्बन्ध हुए । उनकी कन्याएँ भारत आयीं । सत्याभामा व शैव्या के प्रसंग यही बताते है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सारी धरित्री पर बसे विश्व के सारे मानव आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व तक भारतीय संस्कृति के ही अनुयायी इसी की संतति थे । भारतीय दृष्टि से वे संस्कारच्युत थे किन्तु बहुसंख्य सतत् प्रयत्नशील रहते थे कि वे भारतीय आचारधारा के संपर्क में रहें । भारतीय नृतत्वविज्ञान के अन्वेषणकर्ता श्रीटेलर कहते हैं कि विश्व में ईरान की पारसी जाती और भारतवासी हिन्दू यही प्राचीनतम संस्कृतियों के उपासक मूलत: हैं । दोनों अपना निवास मूलत: हिमालय को मानते हैं । पारसी धर्म से ही क्रमश: यहूदी, ईसाई, मुसलमान धर्म विकसित हुए । बौद्धधर्म हिन्दू धर्म की ही एक शाखा है और जैन धर्म की भाँति हिन्दू धर्म से ही वह उत्पन्न हुआ है । इन सभी को मत-सम्प्रदाय कहा जाय तो उचित होगा । मूलतह एक ही है वैदिक धर्म-हिन्दू धर्म । पारसी धर्म इस वैदिक धर्म से ही निकला है, इस पर सभी अन्वेषक सहमत हैं । भारत से बाहर जाकर बसी एक आर्यों की शाखा पारस्य देश (फारस) में बस गयी व पारसी बनकर भारत व अन्यान्य-क्षेत्रों को गयी । फारसी में च्सज् का उच्चारण च्हज् होता है अत: उन्होंने सिंधु देश को हिन्दू कहा, स्वयं को पश्चिमी हिन्दू तथा भारतीयों को पूर्वी हिन्दू कहा । अपनी नदी-नगरों के नाम भी उन्होंने संस्कृतनिष्ठ रखे । सरस्वती वहाँ हरहवती कहलायी, सरयू हरयू तथा भारत यूफरत (यूफ्रेटिस) भूपालन बेबिलोन तथा काशी कास्सी बन गए । अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा ही पारसी धर्म की मूल है इस तथ्य पर सभी वैदिक साहित्यकार व अन्वेषक एकमत हैं । गोपथ ब्राह्मण में शन्नो देवी इस मंत्र से अथर्ववेद पढऩा चाहिए यह बात 1.19 मंत्र बतायी गयी है । पारसी धर्मग्रन्थ होमयस्त के 1.24 मंत्र में यही बात कही गयी है । इस प्रकार ईसाई इस्लाम सभी धर्म वैदिक धर्म से जन्मे, ही प्रमाणित है । यहाँ उद्देश्य किसी प्रकार का साम्प्रदायिक विद्वेष खड़ा करना व अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने का नहीं, वरन् देवसंस्कृति के विराट सामयिक रूप का परिचय देना है, जिसका मूल खोजने पर हुई शोध हमें च्ज्एकं सद्विप्र बहुधा वदन्तिज्ज् का संदेश देकर एक ही सत्ता को परमसत्ता मानने की प्रेरणा देती है । नृतत्व विज्ञान से लेकर चिरपुरातन इतिहास का आमूलचूल सवेर्क्षण एक ही तथ्य प्रामणित करता है कि आदिकालीन मानव आर्य था,वैदिक धर्म को मानता था व चिंतन चरित्र व व्यवहार की दृष्टि से श्रेष्ठ था । शक , हूण, मिस्त्री, यवन आदि सब हिन्दू ही थे । कालान्तर में संस्कार विहीन होने के कारण ये जातियाँ आयार्वत्त से बाहर जाती रहीं, निवार्सित होती रहीं, पुन: मातृदेश लौटती रहीं । पुरातन काल में जातिच्युत व्यक्ति को पुन: आर्य-मानव जाति का अंग बना लेना ही शुद्ध का प्रतीक था । जाति की मिथ्या परिभाषा, वर्ण जातिभेद की गलत व्याख्याएँ तथा व्यापक पैमाने पर बहिष्कार की परम्परा ने हिन्दू संस्कृति का कालान्तर में कितना नुकसान किया व आज भी विश्व मानवता के पथ पर एक अवरोध बनकर खड़ा है, इस पर सभी मानवतावादियों का मत एक है । हमारें प्राचीन संतों-मनीषियों ने हिन्दू संस्कृति को देवसंस्कृति कहकर उसके चिरपुरातन गौरव की ओर ध्यान दिए जाने को तो हम सबसे कहा पर साथ ही यह भी निदेर्श दिया कि हमारी संस्कृति में कालक्रम के अनुसार कई विकृतियां का समावेश होता रहा है । हमें युगानुकूल संस्कृति विकसित करना है व इसे विज्ञान सम्मत, पुन: इसके शाश्वत सावर्जनीन रूप में लाकर इसके द्वारा विश्वमानवता का मागर्दशर्न करना है ।
अभगच्छत राजेन्द्र देविकां विश्रुताम् । प्रसूर्तित्र विप्राणां श्रूयते भरतर्षभ॥
अर्थात्-सप्तचरुतीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई । प्रमाण यही बताते हैं कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति भारत के उत्तराखण्ड अर्थात् इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ही हुई ।
संसार भर में गोरे, पीले, लाल और श्याम (काले) ये चार रंगो के लोग विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं । एक भारत ही ऐसा देश है, जहाँ, इन चार रंगो का भरपूर मिश्रण एक साथ देखने को मिलता है । वस्तुत: श्वेत-काकेशस, पीले-मंगोलियन, काले-नीग्रो तथा लाल रेड इंडियन इन चार प्रकार के रंगविभाजनों के बाद वाँचवी मूल एवं पुख्य नस्ल है, जो भारतीय कहलाती है । इस जाति में उर्पयुक्त चारों का सम्मिश्रण है । ऐसा कहीं सिद्ध नहीं होता कि भारतीय मानव जाति उर्पयुक्त चारों जातियों की वर्ण संकरता से उत्पन्न हुई । उलटे नृतत्व विज्ञानी यह कहते हैं कि भारतीय सम्मिश्रण वर्ण ही यहाँ से विस्तरित होकर दीर्घकाल में जलवायु आदि के भेद से चार मुख्य रूप लेता चला गया । न केवल रंग यहाँ चारों के सम्मिश्रण पाए जाते हैं, वरन् भारतीयों का शारीरिक गठन भी एक विलक्षणता लिए है । ऊँची दबी, गोल-लम्बी मस्तकाकृति उठी या चपटी नाक लम्बी-ठगनी, पतली मोटी शरीराकृत, एक्जों व एण्डोमॉर्फिक (एकहरी या दुहरी गठन वाली) आकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं । यहाँ से अन्यत्र बस जाने पर इनके जो गुण सूत्र उस जलवायु में प्रभावी रहे, वे काकेशस, मंगोलियन, नीग्रॉइड व रेडइंडियन्स के रूप में विकसित होते चले गए । अत: मूल आर्य जाति की उत्पत्ति स्थली भारत ही है, बाहर कहीं नहीं, यह स्पष्ट तथ्य एक हाथ लगता है । पाश्चात्य विद्वानों ने एक प्रचार किया कि आर्य भारत से कहीं बाहर विदेश से आकर यहाँ बसे थे । संभवत: इसके साथ दूसरी निम्न जातियों को जनजाति-आदिवासी वर्ग का बताकर, वे उन्हें उच्च वर्ग के विरुद्ध उभारना चाहते थे । द्रविड़ तथा कोल, ये जो दो जातियाँ भारत में बाहर से आईं बतायी जाती हैं, वस्तुत: आर्य जाति से ही उत्पन्न हुई थीं, इनकी एक शाखा जो बाहर गयी थी पुन: भारत वापस आकर यहाँ बस गयी । भारतीय जातियों पर शोध करने वाले नतृत्व विज्ञानी श्रीनैफील्ड लिखते हैं कि भारत में बाहर से आए आर्य विजेता और मूल आदिम मानव (अरबोरिजिन) जैसे कोई विभाजन नही है । ये विभाग सर्वथा आधुनिक हैं । यहाँ तो समस्त भारतीयों में एक विलक्षण स्तर की एकता है । ब्राह्मणों से लेकर सड़क साफ करने वाले भंगियों तक की आकृति और रक्त समान हैं ।
मनुसंहिता(1(/43-44)का एक उदाहरण है
शनकैस्तु क्रियालोपदिना: क्षत्रिय जातय: । वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च॥
पौण्ड्रकाशचौण्ड्रद्रविडा: काम्बोजा: भवना: शका: । पारदा: पहल्वाश्चीना: किरता: दरदा: खशा:॥
अर्थात् ब्राह्मणत्व की उपलब्धि को प्राप्त न होने के कारण उस क्रिया का लोप होने से पोण्ड्र, चौण्ड्र, द्रविड़ काम्बोज, भवन, शक पारद, पहल्व, चीनी किरात, दरद व खश ये क्षत्रिय जातियाँ धीरे-धीरे शूद्रत्व को प्राप्त हो गयीं । स्मरण रहे यहाँ ब्राह्मणत्व से तात्पर्य है श्रेष्ठ चिन्तन, ज्ञान का उपार्जन व श्रेष्ठ कर्म तथा शूद्रत्व से अर्थ है निकृष्ट चिंतन व निकृष्ट कर्म । क्षत्रिय वे जो पुरुषार्थी थे व बाहुबल से क्षेत्रों की विजय करके राज्य स्थापना हेतु बाहर जाते रहे । मूल आर्य जाति ने उत्तराखण्ड से नीचे की भूमि में वनों को काटकर, जलाकर उन्हें रहने योग्य बनाया । वहाँ नगर बसाये । इससे पूर्व वहाँ कोई निवास नहीं करता था । इस प्रकार मूल निवासी के रूप में एक ही उत्पत्ति आर्यों के रूप में हिमालय के उत्तराखण्ड क्षेत्र में हुई । वहीं से मनुष्य जाति का सारे विश्व में विस्तार हुआ । आदि मानव हिन्दू समाज था । इस प्रकार शेष सभी धर्म-मत-जातियाँ-रेस-वर्ण कालान्तर में समय प्रवाह के साथ विकसित होते चले गए भारतीय आर्षग्रन्थ ऋग्वेद केवल भारतीय आर्यों की ही नहीं बल्कि विश्वभर के आर्यों (श्रेष्ठ मानवों) की सबसे प्राचीन पुस्तक है । मनुसंहिता यही बात कहती है-
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानव:॥
किन्तु भारत से बाहर जाने के बावजूद अपने धर्म आचरण के प्रति अनुराग के उनने अपने सम्बन्ध भारतवर्ष से बनाए रखे । महाभारत काल तक भारतीय नरेशों से उनके वैवाहिक सम्बन्ध हुए । उनकी कन्याएँ भारत आयीं । सत्याभामा व शैव्या के प्रसंग यही बताते है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सारी धरित्री पर बसे विश्व के सारे मानव आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व तक भारतीय संस्कृति के ही अनुयायी इसी की संतति थे । भारतीय दृष्टि से वे संस्कारच्युत थे किन्तु बहुसंख्य सतत् प्रयत्नशील रहते थे कि वे भारतीय आचारधारा के संपर्क में रहें । भारतीय नृतत्वविज्ञान के अन्वेषणकर्ता श्रीटेलर कहते हैं कि विश्व में ईरान की पारसी जाती और भारतवासी हिन्दू यही प्राचीनतम संस्कृतियों के उपासक मूलत: हैं । दोनों अपना निवास मूलत: हिमालय को मानते हैं । पारसी धर्म से ही क्रमश: यहूदी, ईसाई, मुसलमान धर्म विकसित हुए । बौद्धधर्म हिन्दू धर्म की ही एक शाखा है और जैन धर्म की भाँति हिन्दू धर्म से ही वह उत्पन्न हुआ है । इन सभी को मत-सम्प्रदाय कहा जाय तो उचित होगा । मूलतह एक ही है वैदिक धर्म-हिन्दू धर्म । पारसी धर्म इस वैदिक धर्म से ही निकला है, इस पर सभी अन्वेषक सहमत हैं । भारत से बाहर जाकर बसी एक आर्यों की शाखा पारस्य देश (फारस) में बस गयी व पारसी बनकर भारत व अन्यान्य-क्षेत्रों को गयी । फारसी में च्सज् का उच्चारण च्हज् होता है अत: उन्होंने सिंधु देश को हिन्दू कहा, स्वयं को पश्चिमी हिन्दू तथा भारतीयों को पूर्वी हिन्दू कहा । अपनी नदी-नगरों के नाम भी उन्होंने संस्कृतनिष्ठ रखे । सरस्वती वहाँ हरहवती कहलायी, सरयू हरयू तथा भारत यूफरत (यूफ्रेटिस) भूपालन बेबिलोन तथा काशी कास्सी बन गए । अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा ही पारसी धर्म की मूल है इस तथ्य पर सभी वैदिक साहित्यकार व अन्वेषक एकमत हैं । गोपथ ब्राह्मण में शन्नो देवी इस मंत्र से अथर्ववेद पढऩा चाहिए यह बात 1.19 मंत्र बतायी गयी है । पारसी धर्मग्रन्थ होमयस्त के 1.24 मंत्र में यही बात कही गयी है । इस प्रकार ईसाई इस्लाम सभी धर्म वैदिक धर्म से जन्मे, ही प्रमाणित है । यहाँ उद्देश्य किसी प्रकार का साम्प्रदायिक विद्वेष खड़ा करना व अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने का नहीं, वरन् देवसंस्कृति के विराट सामयिक रूप का परिचय देना है, जिसका मूल खोजने पर हुई शोध हमें च्ज्एकं सद्विप्र बहुधा वदन्तिज्ज् का संदेश देकर एक ही सत्ता को परमसत्ता मानने की प्रेरणा देती है । नृतत्व विज्ञान से लेकर चिरपुरातन इतिहास का आमूलचूल सवेर्क्षण एक ही तथ्य प्रामणित करता है कि आदिकालीन मानव आर्य था,वैदिक धर्म को मानता था व चिंतन चरित्र व व्यवहार की दृष्टि से श्रेष्ठ था । शक , हूण, मिस्त्री, यवन आदि सब हिन्दू ही थे । कालान्तर में संस्कार विहीन होने के कारण ये जातियाँ आयार्वत्त से बाहर जाती रहीं, निवार्सित होती रहीं, पुन: मातृदेश लौटती रहीं । पुरातन काल में जातिच्युत व्यक्ति को पुन: आर्य-मानव जाति का अंग बना लेना ही शुद्ध का प्रतीक था । जाति की मिथ्या परिभाषा, वर्ण जातिभेद की गलत व्याख्याएँ तथा व्यापक पैमाने पर बहिष्कार की परम्परा ने हिन्दू संस्कृति का कालान्तर में कितना नुकसान किया व आज भी विश्व मानवता के पथ पर एक अवरोध बनकर खड़ा है, इस पर सभी मानवतावादियों का मत एक है । हमारें प्राचीन संतों-मनीषियों ने हिन्दू संस्कृति को देवसंस्कृति कहकर उसके चिरपुरातन गौरव की ओर ध्यान दिए जाने को तो हम सबसे कहा पर साथ ही यह भी निदेर्श दिया कि हमारी संस्कृति में कालक्रम के अनुसार कई विकृतियां का समावेश होता रहा है । हमें युगानुकूल संस्कृति विकसित करना है व इसे विज्ञान सम्मत, पुन: इसके शाश्वत सावर्जनीन रूप में लाकर इसके द्वारा विश्वमानवता का मागर्दशर्न करना है ।
समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान
भारत जिसमें कभी तैंतीस कोटि देवता निवास करते थे, जिसे कभी स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता था, एक स्वर्णिम अतीत वाला चिर पुरातन देश है जिसके अनुदानों से विश्व-वसुधा का चप्पा-चप्पा लाभान्वित हुआ है । भारत ने ही अनादि काल से समस्त संसार का मार्ग-दर्शन किया हैं ज्ञान और विज्ञान की समस्त धाराओं का उदय, अवतरण भी सर्वप्रथम इसी धरती पर हुआ पर यह यहीं तक सीमित नहीं रहा-यह सारे विश्व में यहाँ से फैल गया । सोने की चिडिय़ा कहा जाने वाला हमारा भारतवर्ष जिसकी परिधि कभी सारी विश्व-वसुधा थी, आज अपने दो सहस्र वर्षीय अंधकार युग के बाद पुन: उसी गौरव की प्राप्ति की ओर अग्रसर है । ह्यज्ज्सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाराज्ज् यह उक्ति बताती है कि हमारी संस्कृति, हिन्दू संस्कृति देव संस्कृति, ही सर्व प्रथम वह संस्कृति थी जो सभी विश्वभर में फैल गयी । अपनी संस्कृति पर गौरव जिन्हें होना चाहिए वे ही भारतीय यदि इस तथ्य से विमुख होकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर उन्मुख होने लगें तो इसे एक विडम्बना ही कहा जायगा । इसी तथ्य पर सर्वाधिकार जोर देते हुए पूज्यवर ने लिखा है कि जिस देश का अतीत इतना गौरवमय रहा हो, जिसकी इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पुण्य परम्पराएँ रहीं हों, उसे अपने पूर्वजों को न भुलाकर अपना चिन्तन और कर्तृत्त्व वैसा ही बनाकर देवोपम स्तर का जीवन जीना चाहिए । वसतुत: सांस्कृतिक मूल्य ही किसी राष्ट की प्रगति अवगति का आधार बनते हैं । जब इनकी अवमानना होती है तो राष्ट पतन की ओर जाने लगता है । संस्कृति के उत्थान में रहा है । जब-जब यह परिष्कृति रहा है, तब-तब इसने राष्ट ही नहीं, विश्व भर की समस्त सभ्यताओं को विकास मार्ग दिखाया है । आज भी ऐसे परिष्कृति धर्मतंत्र विज्ञान सम्भव उन प्रतिपादनों पर टिका है जो संस्कृति के प्रत्येक निर्धारण की उपयोगिता प्रतिपादित करते हैं । इन्हीं सब का विवेचन इस खण्ड में हैं । पुरातन भारत का ज्ञान-विज्ञान आज के वैज्ञानिक युग की उपलब्धियों को भी चुनौती देने में सक्षम हैं । हमारी वैदिक संस्कृति में वह सब है जो आज का अणु विज्ञान हमें बताता है । इस धरोवर को भले ही हमने भुला दिया हो किन्तु वह हमें सतत याद दिलाती रहती है वेदों की अपनी विज्ञान सम्मत सूत्र शैली के माध्यम से । हमारी संस्कृति की जितनी मान्यताएँ हैं उन्हें पूज्यवर ने विज्ञान की कसौटी पर कस कर प्रमाणों के साथ उनको आज के विज्ञान समुदाय के समक्ष रखा है । ताकि पाश्चात्य प्रभाव में पनप रही पीढ़ी कहीं उन्हें एक दम भुला न दे । हमारे स्वर्णिम अतीत पर एक दृष्टि डालते हुए इस खण्ड में यह सब विस्तार में लिखा गया है कि प्रवज्या-तीर्थ यात्रा के माध्यम से हमारी संस्कृति का विस्तार प्राचीन काल में कहाँ-कहाँ तक हुआ था । अमेरिका, लातिनी अमेरिका, मेक्सिको, जर्मनी, जिसे यूरोप का आर्यावर्त कहा जाता है, मिश्र से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक, कम्पूचिया, लाओस, चीन, जापान आदि देशों में स्थान-स्थान पर ऐसे अवशेष विद्यमान हैं जो बताते हैं कि आदिकाल में वहाँ भारतीय संस्कृति का ही साम्राज्य था । इसके लिए परमपूज्य गुरुदेव ने विभन्न पाश्चात्य विद्वानों का हवाला देकर हमारे पुराने-शास्त्र ग्रन्थों के उद्धरण के साथ विस्तृत विवेचन किया है । यह विस्तार मात्र धार्मिक ही नहीं था अपितु, विश्व राष्ट की आर्य-व्यवस्था, शासन संचालन-व्यवस्था, कला उद्योग, शिल्प आदि सभी में भारतीय-संस्कृति का योगदान रहा है । मॉरीशस, आस्टे्रलिया, फिजी व अन्य प्रशांत महासागर के छोटे-छोटे द्वीप, रूस, कोरिया, मंगोलिया, इण्डोनेशिया, श्याम देश आदि के विस्तृत उदाहरणों से हमें भारतीय संस्कृति के विश्व संस्कृति होने की एक झलक मिलती है । अन्यान्य सभी देशों में भारतीय संस्कृति के अस्तित्व का परिचय देते हुए यह खण्ड प्रवासी भारतीयों के संगठनों की जानकारी हमें विस्तार से देता है जो विदेश में भारत की एक बहुमूल्य पूँजी के रूप में बैठे सांस्कृतिक दूत का कार्य कर रहे हैं । भारतीय संस्कृति इन्हीं के माध्यम से कभी विश्वभर में फैली थी, आज भी विश्व में इन्हीं के द्वारा फैलेगी । भारतीय संस्कृति के विराट विस्तार एवं वृहत्तर भारत जो कभी था व कभी आगे चलकर बनेगा, उसकी जानकारी पाने पर प्रत्येक को अपने देश की एतिहासिक परम्परा व सांस्कृतिक विरासत पर गौरव होता है व अपने र्कत्तव्य का ज्ञान भी कि हम कैसे इसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं । निश्चित ही देव संस्कृति के विश्व संस्कृति के रूप में विस्तार की जानकारी देने में यह खण्ड महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा हमारा विश्वास हैं ।
भारत के प्राचीन शिक्षा केन्द्र
प्राचीन काल से ही हमारे देश में शिक्षा का बहुत महत्व रहा है। प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण संसार में सुविख्यात थे। इन विश्वविद्यालयों में देश ही नहीं विदेश के विद्यार्थी भी अध्ययन के लिए आते थे। इन शिक्षा केन्द्रों की अपनी विशेषताएं थीं जिनका वर्णन प्रस्तुत है-
तक्षशिला विश्वविद्यालय — तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिण्डी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्विद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहां 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकन्दर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केन्द्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई एक केन्द्रीय स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तृत भू भाग में फैला हुआ था। विविध विद्याओं के विद्वान आचार्यो ने यहां अपने विद्यालय तथा आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचिनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। महत्वपूर्ण पाठयक्रमों में यहां वेद-वेदान्त, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्धविद्या, शस्त्र-संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व-विद्या, मन्त्र-विद्या, विविद्य भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनी, कौटिल्य, चन्द्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट पाठयक्रम था। आज कल की तरह पाठयक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी और न कोई विशिष्ट प्रमाणपत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे। परंतु कहीं-कहीं कुछ पाठयक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के कुछ पाठयक्रम सात वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को छ: माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी-बूटी पता लगाता तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। अनेक शोधों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहां बारह वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। 500 ई. पू. जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केन्द्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहां के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा अंतडिय़ों तक का आपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी-बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्राय: सौ से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहां धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्रा आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। प्राचीन साहित्य से विदित होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढऩे वाले उच्च वर्ण के ही छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। उसके बाद यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी, जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ई. पू. से ही इस मार्ग से भारत वर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई। अंतत: छठवीं शताब्दी में यह आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया।
नालन्दा विश्वविद्यालय — नालन्दा विश्वविद्यालय बिहार में राजगीर के निकट रहा है और उसके अवशेष बडगांव नामक गांव व आस-पास तक बिखरे हुए हैं। पहले इस जगह बौद्ध विहार थे। इनमें बौद्ध साहित्य और दर्शन का विशेष अध्ययन होता था। बौद्ध ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख है कि नालन्दा के क्षेत्र को पांच सौ सेठों ने एक करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं में खरीदकर भगवान बुद्ध को अर्पित किया था। महाराज शकादित्य (सम्भवत: गुप्तवंशीय सम्राट कुमार गुप्त, 415-455 ई.) ने इस जगह को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अन्य राजाओं ने यहां अनेक विहारों और विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण करवाया। इनमें से गुप्त सम्राट बालादित्य ने 470 ई. में यहां एक सुंदर मंदिर बनवाकर भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा स्थापित की थी। देश के विद्यार्थियों के अलावा कोरिया, चीन, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों के विद्यार्थी शिक्षा लेने यहां आते थे। विदेशी यात्रियों के वर्णन के अनुसार नालन्दा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने की उत्तम व्यवस्था थी। उल्लेख मिलता है कि यहां आठ शालाएं और 300 कमरे थे। कई खंडों में विद्यालय तथा छात्रावास थे। प्रत्येक खंड में छात्रों के स्नान लिए सुंदर तरणताल थे जिनमें नीचे से ऊपर जल लाने का प्रबंध था। शयनस्थान पत्थरों के बने थे। जब नालन्दा विश्वविद्यालय की खुदाई की गई तब उसकी विशालता और भव्यता का ज्ञान हुआ। यहां के भवन विशाल, भव्य और सुंदर थे। कलात्मकता तो इनमें भरी पड़ी थी। यहां तांबे एवं पीतल की बुद्ध की मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। नालन्दा विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने ज्ञान एवं विद्या के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। इनका चरित्र सर्वथा उज्जवल और दोषरहित था। छात्रों के लिए कठोर नियम था। जिनका पालन करना आवश्यक था। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया था। उसने दस वर्षों तक यहां अध्ययन किया। उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। यहां केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश के लिए पहले छात्र को परीक्षा देनी होती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय के छ: द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर एक द्वार पण्डित होता था। प्रवेश से पहले वो छात्रों की वहीं परीक्षा लेता था। इस परीक्षा में 20 से 30 प्रतिशत छात्र ही उत्तीर्ण हो पाते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी छात्रों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था तथा अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। यहां से स्नातक करने वाले छात्र का हर जगह सम्मान होता था। हर्ष के शासनकाल में इस विश्वविद्यालय में दस हजार छात्र पढ़ते थे। हेनसांग के अनुसार यहां अनेक भवन बने हुए थे। इनमें मानमंदिर सबसे ऊंचा था। यह मेघों से भी ऊपर उठा हुआ था। इसकी कारीगरी अद्भुत थी। नालन्दा विश्वविद्यालय के तीन भवन मुख्य थे- रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। नालन्दा का केन्द्रीय पुस्तकालय इन्हीं भवनों में स्थित था। इनमें रत्नोदधि सबसे विशाल था। इसमें धर्म-ग्रंथों का विशेष संग्रह था। अन्य भवनों में विविध विषयों के दुर्लभ-ग्रंथों का संग्रह था। नालन्दा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं नि:शुल्क थीं। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिये गये दान से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों की कीर्ति विदेशों में विख्यात थी और उनको वहां बुलाया जाता था। आठवीं शताब्दी में शान्तरक्षित नाम के आचार्य को तिब्बत बुलाया गया था। उसके बाद कमलशील और अतिशा नाम के विद्वान भी वहां गये। नालन्दा विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी तक यानि लगभग 800 वर्षों तक विश्व में ज्ञान का प्रमुख केन्द्र बना रहा। इसी समय यवनों के आक्रमण शुरु हो गये। इतिहास बताता है कि खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर यहां के हजारों छात्रों और अधयापकों को कत्ल करवा दिया। इसके पुस्तकालय में आग लगा दी गई। छ: महीनों तक पुस्तकालयों की पुस्तकें जलती रहीं जिससे दस हजार की सेना का मांसाहारी भोजन बनता रहा। इस घटना से भारत ने ही नहीं संसार ने भी ज्ञान का भंडार खो दिया।
विक्रमशील विश्वविद्यालय — विक्रमशील विश्विद्यालय की स्थापना 8-9वीं शताब्दी ई. में बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। वह बौद्ध था। प्रारंभ इस विश्वविद्यालय का विकास भी नालंदा विश्विद्यालय की तरह बौद्ध विहार के रूप में ही हुआ था। यह वर्तमान भागलपुर से 24 मील दूर पर निर्मित था। इस विश्वविद्यालय के छात्रों को भी सारी सुविधाएं नि:शुल्क दी जाती थीं। धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय में उस समय के विख्यात दस आचार्यों की नियुक्ति की थी। कालान्तर में इसकी संख्या में वृद्धि हुई। यहां छ: विद्यालय बनाये गये थे। प्रत्येक विद्यालय का एक पण्डित होता था, जो प्रवेश परीक्षा लेता था। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। प्रत्येक विद्यालय में 108 शिक्षक थे। इस प्रकार कुल शिक्षकों की संख्या 648 बताई जाती है। दसवीं शताब्दी ई. में तिब्बती लेखक तारानाथ के वर्णन के अनुसार प्रत्येक द्वार के पण्डित थे। पूर्वी द्वार के द्वार पण्डित रत्नाकर शान्ति, पश्चिमी द्वार के वर्गाश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार के नारोपन्त, दक्षिणी द्वार के प्रज्ञाकरमित्रा थे। आचार्य दीपक विक्रमशील विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रसिद्ध आचार्य हुये हैं। विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या का सही अनुमान प्राप्त नहीं हो पाया है। 12वीं शताब्दी में यहां 3000 छात्रों के होने का विवरण प्राप्त होता है। लेकिन यहां के सभागार के जो खण्डहर मिले हैं उनसे पता चलता है कि सभागार में 8000 व्यक्तियों को बिठाने की व्यवस्था थी। विदेशी छात्रों में तिब्वती छात्रों की संख्या अधिक थी। एक छात्रावास तो केवल तिब्बती छात्रों के लिए ही था। विक्रमशील विश्वविद्यालय में मुख्यत: बौद्ध साहित्य के अध्ययन के साथ-साथ वैदिक साहित्य के अध्ययन का भी प्रबंध था। इनके अलावा विद्या के अन्य विषय भी पढ़ाये जाते थे। बौद्धों के वज्रयान सम्प्रदाय के अध्ययन का यह प्रामाणिक केन्द्र रहा। 12वीं शताब्दी तक विक्रमशील विश्विद्यालय अपने ज्ञान के आलोक से संपूर्ण विश्व को जगमगाता रहा। नालन्दा विश्वविद्यालय को नष्ट करके मुहम्मद खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को भी पूर्णत: नष्ट कर दिया।
उड्डयन्तपुर विश्वविद्यालय —
इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रवर्तक तथा प्रथम राजा गोपाल ने की थी। इसकी स्थापना भी बौद्ध विहार के रूप में हुई थी। आज यहां बिहार नगर है। पहले यह क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में यह शिक्षा का अच्छा केन्द्र था। यहां हजारों अध्यापक और छात्र निवास करते थे। अनंत एवं समुचित सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं थीं। इसके विशाल भवनों को देखकर खिलजी ने समझा कि यह कोई दुर्ग है। उसने इस पर आक्रमण कर दिया। राजाओं ने तथा उनकी सेनाओं ने इसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। विश्वविद्यालय के छात्रों और आचार्यों ने आक्रमणकारियों से मुकाबला किया। परंतु खिलजी की विशालकाय सेना के आगे वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाये। खिलजी ने सभी की क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी। जब सभी आचार्य एवं छात्र मारे गये तब जाकर अफगानों का इस पर अधिकार हो पाया। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह खिजली की सेना ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को भी जला दिया।
इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सौराष्ट्र बलभी विश्वविद्यालय भी काफी प्रसिद्ध रहा है। अन्य असंख्य शिक्षा केन्द्र भारतवर्ष के कोने-कोने में स्थित थे। 317 ई. पू. तमिलनाडु में मदुराई विद्या एवं शिक्षण संस्थानों का केन्द्र रहा है। सुप्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर यहां के छात्र थे। उलवेरूनी के अनुसार 11वीं शताब्दी ई. में कश्मीर विद्या का केन्द्र रहा था। इसी शताब्दी के अंतिम भाग में बंगाल के राजा रामपाल ने रामावती नगरी में जगद्धर विहार की स्थापना की थी। उस समय प्राय: प्रत्येक मठ और विहार शिक्षा के केन्द्र होते थे। शंकराचार्य ने वैदिक विषयों के अध्ययन के लिए अनेक विद्यालयों की स्थापना की। ये मठों के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी, कांची, मथुरा, पुरी आदि तीर्थस्थान भी विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र रहे हैं।
तक्षशिला विश्वविद्यालय — तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिण्डी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्विद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहां 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकन्दर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केन्द्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई एक केन्द्रीय स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तृत भू भाग में फैला हुआ था। विविध विद्याओं के विद्वान आचार्यो ने यहां अपने विद्यालय तथा आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचिनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। महत्वपूर्ण पाठयक्रमों में यहां वेद-वेदान्त, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्धविद्या, शस्त्र-संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व-विद्या, मन्त्र-विद्या, विविद्य भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनी, कौटिल्य, चन्द्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट पाठयक्रम था। आज कल की तरह पाठयक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी और न कोई विशिष्ट प्रमाणपत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे। परंतु कहीं-कहीं कुछ पाठयक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के कुछ पाठयक्रम सात वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को छ: माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी-बूटी पता लगाता तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। अनेक शोधों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहां बारह वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। 500 ई. पू. जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केन्द्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहां के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा अंतडिय़ों तक का आपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी-बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्राय: सौ से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहां धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्रा आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। प्राचीन साहित्य से विदित होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढऩे वाले उच्च वर्ण के ही छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। उसके बाद यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी, जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ई. पू. से ही इस मार्ग से भारत वर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई। अंतत: छठवीं शताब्दी में यह आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया।
नालन्दा विश्वविद्यालय — नालन्दा विश्वविद्यालय बिहार में राजगीर के निकट रहा है और उसके अवशेष बडगांव नामक गांव व आस-पास तक बिखरे हुए हैं। पहले इस जगह बौद्ध विहार थे। इनमें बौद्ध साहित्य और दर्शन का विशेष अध्ययन होता था। बौद्ध ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख है कि नालन्दा के क्षेत्र को पांच सौ सेठों ने एक करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं में खरीदकर भगवान बुद्ध को अर्पित किया था। महाराज शकादित्य (सम्भवत: गुप्तवंशीय सम्राट कुमार गुप्त, 415-455 ई.) ने इस जगह को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अन्य राजाओं ने यहां अनेक विहारों और विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण करवाया। इनमें से गुप्त सम्राट बालादित्य ने 470 ई. में यहां एक सुंदर मंदिर बनवाकर भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा स्थापित की थी। देश के विद्यार्थियों के अलावा कोरिया, चीन, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों के विद्यार्थी शिक्षा लेने यहां आते थे। विदेशी यात्रियों के वर्णन के अनुसार नालन्दा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने की उत्तम व्यवस्था थी। उल्लेख मिलता है कि यहां आठ शालाएं और 300 कमरे थे। कई खंडों में विद्यालय तथा छात्रावास थे। प्रत्येक खंड में छात्रों के स्नान लिए सुंदर तरणताल थे जिनमें नीचे से ऊपर जल लाने का प्रबंध था। शयनस्थान पत्थरों के बने थे। जब नालन्दा विश्वविद्यालय की खुदाई की गई तब उसकी विशालता और भव्यता का ज्ञान हुआ। यहां के भवन विशाल, भव्य और सुंदर थे। कलात्मकता तो इनमें भरी पड़ी थी। यहां तांबे एवं पीतल की बुद्ध की मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। नालन्दा विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने ज्ञान एवं विद्या के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। इनका चरित्र सर्वथा उज्जवल और दोषरहित था। छात्रों के लिए कठोर नियम था। जिनका पालन करना आवश्यक था। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया था। उसने दस वर्षों तक यहां अध्ययन किया। उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। यहां केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश के लिए पहले छात्र को परीक्षा देनी होती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय के छ: द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर एक द्वार पण्डित होता था। प्रवेश से पहले वो छात्रों की वहीं परीक्षा लेता था। इस परीक्षा में 20 से 30 प्रतिशत छात्र ही उत्तीर्ण हो पाते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी छात्रों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था तथा अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। यहां से स्नातक करने वाले छात्र का हर जगह सम्मान होता था। हर्ष के शासनकाल में इस विश्वविद्यालय में दस हजार छात्र पढ़ते थे। हेनसांग के अनुसार यहां अनेक भवन बने हुए थे। इनमें मानमंदिर सबसे ऊंचा था। यह मेघों से भी ऊपर उठा हुआ था। इसकी कारीगरी अद्भुत थी। नालन्दा विश्वविद्यालय के तीन भवन मुख्य थे- रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। नालन्दा का केन्द्रीय पुस्तकालय इन्हीं भवनों में स्थित था। इनमें रत्नोदधि सबसे विशाल था। इसमें धर्म-ग्रंथों का विशेष संग्रह था। अन्य भवनों में विविध विषयों के दुर्लभ-ग्रंथों का संग्रह था। नालन्दा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं नि:शुल्क थीं। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिये गये दान से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों की कीर्ति विदेशों में विख्यात थी और उनको वहां बुलाया जाता था। आठवीं शताब्दी में शान्तरक्षित नाम के आचार्य को तिब्बत बुलाया गया था। उसके बाद कमलशील और अतिशा नाम के विद्वान भी वहां गये। नालन्दा विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी तक यानि लगभग 800 वर्षों तक विश्व में ज्ञान का प्रमुख केन्द्र बना रहा। इसी समय यवनों के आक्रमण शुरु हो गये। इतिहास बताता है कि खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर यहां के हजारों छात्रों और अधयापकों को कत्ल करवा दिया। इसके पुस्तकालय में आग लगा दी गई। छ: महीनों तक पुस्तकालयों की पुस्तकें जलती रहीं जिससे दस हजार की सेना का मांसाहारी भोजन बनता रहा। इस घटना से भारत ने ही नहीं संसार ने भी ज्ञान का भंडार खो दिया।
विक्रमशील विश्वविद्यालय — विक्रमशील विश्विद्यालय की स्थापना 8-9वीं शताब्दी ई. में बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। वह बौद्ध था। प्रारंभ इस विश्वविद्यालय का विकास भी नालंदा विश्विद्यालय की तरह बौद्ध विहार के रूप में ही हुआ था। यह वर्तमान भागलपुर से 24 मील दूर पर निर्मित था। इस विश्वविद्यालय के छात्रों को भी सारी सुविधाएं नि:शुल्क दी जाती थीं। धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय में उस समय के विख्यात दस आचार्यों की नियुक्ति की थी। कालान्तर में इसकी संख्या में वृद्धि हुई। यहां छ: विद्यालय बनाये गये थे। प्रत्येक विद्यालय का एक पण्डित होता था, जो प्रवेश परीक्षा लेता था। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। प्रत्येक विद्यालय में 108 शिक्षक थे। इस प्रकार कुल शिक्षकों की संख्या 648 बताई जाती है। दसवीं शताब्दी ई. में तिब्बती लेखक तारानाथ के वर्णन के अनुसार प्रत्येक द्वार के पण्डित थे। पूर्वी द्वार के द्वार पण्डित रत्नाकर शान्ति, पश्चिमी द्वार के वर्गाश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार के नारोपन्त, दक्षिणी द्वार के प्रज्ञाकरमित्रा थे। आचार्य दीपक विक्रमशील विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रसिद्ध आचार्य हुये हैं। विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या का सही अनुमान प्राप्त नहीं हो पाया है। 12वीं शताब्दी में यहां 3000 छात्रों के होने का विवरण प्राप्त होता है। लेकिन यहां के सभागार के जो खण्डहर मिले हैं उनसे पता चलता है कि सभागार में 8000 व्यक्तियों को बिठाने की व्यवस्था थी। विदेशी छात्रों में तिब्वती छात्रों की संख्या अधिक थी। एक छात्रावास तो केवल तिब्बती छात्रों के लिए ही था। विक्रमशील विश्वविद्यालय में मुख्यत: बौद्ध साहित्य के अध्ययन के साथ-साथ वैदिक साहित्य के अध्ययन का भी प्रबंध था। इनके अलावा विद्या के अन्य विषय भी पढ़ाये जाते थे। बौद्धों के वज्रयान सम्प्रदाय के अध्ययन का यह प्रामाणिक केन्द्र रहा। 12वीं शताब्दी तक विक्रमशील विश्विद्यालय अपने ज्ञान के आलोक से संपूर्ण विश्व को जगमगाता रहा। नालन्दा विश्वविद्यालय को नष्ट करके मुहम्मद खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को भी पूर्णत: नष्ट कर दिया।
उड्डयन्तपुर विश्वविद्यालय —
इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रवर्तक तथा प्रथम राजा गोपाल ने की थी। इसकी स्थापना भी बौद्ध विहार के रूप में हुई थी। आज यहां बिहार नगर है। पहले यह क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में यह शिक्षा का अच्छा केन्द्र था। यहां हजारों अध्यापक और छात्र निवास करते थे। अनंत एवं समुचित सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं थीं। इसके विशाल भवनों को देखकर खिलजी ने समझा कि यह कोई दुर्ग है। उसने इस पर आक्रमण कर दिया। राजाओं ने तथा उनकी सेनाओं ने इसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। विश्वविद्यालय के छात्रों और आचार्यों ने आक्रमणकारियों से मुकाबला किया। परंतु खिलजी की विशालकाय सेना के आगे वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाये। खिलजी ने सभी की क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी। जब सभी आचार्य एवं छात्र मारे गये तब जाकर अफगानों का इस पर अधिकार हो पाया। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह खिजली की सेना ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को भी जला दिया।
इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सौराष्ट्र बलभी विश्वविद्यालय भी काफी प्रसिद्ध रहा है। अन्य असंख्य शिक्षा केन्द्र भारतवर्ष के कोने-कोने में स्थित थे। 317 ई. पू. तमिलनाडु में मदुराई विद्या एवं शिक्षण संस्थानों का केन्द्र रहा है। सुप्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर यहां के छात्र थे। उलवेरूनी के अनुसार 11वीं शताब्दी ई. में कश्मीर विद्या का केन्द्र रहा था। इसी शताब्दी के अंतिम भाग में बंगाल के राजा रामपाल ने रामावती नगरी में जगद्धर विहार की स्थापना की थी। उस समय प्राय: प्रत्येक मठ और विहार शिक्षा के केन्द्र होते थे। शंकराचार्य ने वैदिक विषयों के अध्ययन के लिए अनेक विद्यालयों की स्थापना की। ये मठों के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी, कांची, मथुरा, पुरी आदि तीर्थस्थान भी विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र रहे हैं।
सदस्यता लें
संदेश (Atom)