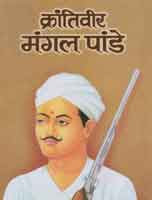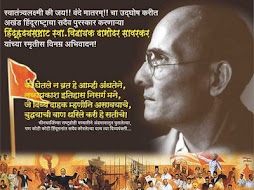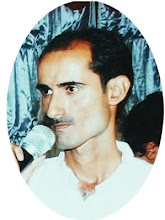गुरुवार, 27 मई 2010
मां तो ऐसी होनी चाहिए
कहते हैं मनुष्य की सबसे पहली शिक्षक मां होती है। इसलिए जरूरी है कि उसका भी एक पाठ्यक्रम हो, ताकि वह एक आदर्श मां बन सके। यानी उसमें इतनी योग्यता हो कि वह अपने बच्चे का हर प्रकार से विकास कर एक सर्वगुण सम्पन्न मानव बना सके। जोकि भविष्य में एक आज्ञाकारी बेटा/बेटी होने के साथ-साथ सच्चा तथा ईमानदार देशभक्त भी बन सके। इस पाठ्यक्रम का सबसे पहला सबक है कि एक मां का उसके बच्चे के जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि वह चाहे तो उसे तराशकर सोना तक बना सकती है। एक पूर्ण मां वह है जो अपने बालक पर जैसा लिख दे वह वैसा ही हो जाए। यथा- मदालसा अपने तीन पुत्रों पर वैरागी लिखती है तो वे वैरागी और एक पर राजा लिखती है तो वह राजा बनता है। इसी प्रकार जीजाबाई अपने पुत्र पर शिवाजी, यशोदा कृष्ण और कौशल्या राम लिखती है, तो वे वही बन जाते हैं। एक महिला के मां बनते ही उसका शिक्षक जीवन शुरू हो जाता है, परन्तु याद रहे एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो सदा शिक्षार्थी भी बना रहे। बालक के धरती पर जन्म लेते ही मां को उसका पाठ्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाए उसका परिचय उसके पिता, दादा-दादी, नाना-नानी आदि परिजनों से कराना। साथ ही उसके वंश से भी उसका परिचय कराना, फिर आगे बढक़र उसका परिचय चंदा, सूरज और ध्रुव से भी कराना। उसका परिचय हिमालय के संयम और अडिगता भी कराना। बालक को यह भी बताना कि वह गंगा की तरह चंचल और सागर की तरह गंभीर रहे। अत: बहुत जरूरी होने पर ही वह अपना संयम तोड़े। उसे यह भी बताना कि वह छायादार वृक्षों की तरह ऊपर की ओर बढ़े, मन में निराशा कभी न लाए। उसे यह भी जरूर बताइए कि वह जिस समाज में रह रहा है, वह क्या, कितना, कहां और कैसा है? उसे यह बताना भी जरूरी है कि हर आदमी का वास्तविक पिता एक ही है और वह परमात्मा है तथा सभी की असली मां यही धरती है। उसे यह भी बताइए कि वह जिन-जिन लोगों की गोद में खेला है, जिनके हाथों में झूला है, वह उन्हें बड़ा होकर भी न भूले। बालक को यह बताना भी जरूरी होगा कि कोई भी जाति अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छा या बुरा तो आदमी होता है। इसलिए जरूरी है कि वह एक अच्छा आदमी बने। उसे यह भी बताना होगा कि वह संसार का सबसे धनिक व्यक्ति होने पर भी संसार के सबसे न्यूनतम स्तर के आदमी जितना ही उपभोग करे। उसे यह भी बताना कि वह खाद्य वस्तुओं को सब में बांटकर खाए। उसे यह भी बताइए कि वह अच्छी और बुरी बातों में भेद करना शुरू करे, यह उसकी प्रगति के लिए अच्छा साबित होगा। उसे बताना होगा कि गलत आदमी को मारने के लिए ही नहीं, बल्कि समझाने के लिए भी शक्तिशाली होना जरूरी है। उसे बताइएगा कि वह जोश में होश कभी न खोए। जीवन में वह शक्ति के संतुलन को भी समझे। उसे यह बताना भी जरूरी है कि उसका सामना गलत रास्तों पर ले जाने वाले गलत लोगों से जरूर होगा और जब ऐसे लोगों से उसका सामना होगा तो उसके साथ कोई नहीं होगा। ऐसे में उसे अकेले ही अपना बचाव करना होगा। उसे जीवन के हर रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करना होगा। उसे सम्पन्नता और विपन्नता में समान रूप से रहने के लिए बताएं। ध्यान रहे उसमें अहंकार के अकुंर कभी भी पैदा न हों। परन्तु सबसे पहले बालक इन सब बातों को अपनी मां में देखना शुरू करेगा। इसलिए मां इसे वास्तव में एक सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति बनाना चाहती है तो इन सब बातों पर अमल करने की उसे स्वयं शुरुआत करनी होगी।
सोमवार, 24 मई 2010
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस : आजादी के महानायक
यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में भारत माता ने ऐसे अनेक नर-पुंगवों को जन्म दिया था, जिनकी तुलना विश्व के किसी अन्य देश से नहीं की जा सकती। किन्तु इसके बावजूद इसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संचालित राष्ट्रीय आन्दोलन की त्रासदीपूर्ण विडम्बना ही कहा जाएगा कि आवेदनकर्ता, उदारवादी, संविधानवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी, जनान्दोलनकारी धाराओं के पुरोधा एक-दूसरे के पूरक न बन सके। फलत: भारत माता को बन्धनमुक्त कराने में केवल एक सुदीर्घ कालखण्ड ही व्यतीत नहीं हुआ, अपितु स्वातंत्र्य देवी का पदार्पण भी मातृभूमि के पातकीय विभाजन के साथ हुआ। इस विषय में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दुनिया के अन्यान्य देशों में 'अन्य नेतागण अपने-अपने देश को कम अनुयायियों के साथ और अल्प कालावधि में स्वतंत्र कराने में सफल रहे हैं। (देखिए, नेताजी-कलेक्टिड वर्क्स, खण्ड-2, 1981, पृष्ठ 329)। इस दुर्भाग्यपर्ण स्थिति का मुख्य कारण वर्ष 1920 में लोकमान्य तिलक के असामयिक निधन के उपरान्त राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन मूलत: पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धान्तों और मनोरचना के आधार पर किया जाना है और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन के मूर्धन्यतम नेता ने अपने से मत-भिन्नता रखने वाले प्रत्येक राजनेता और राजनीतिक समूह को अपना विरोधी मानकर उनको नेस्तोनाबूद करने में अपने प्रयासों की पराकाष्ठा कर दी। एक संक्षिप्त लेख के कलेवर में इस कुचक्र का शिकार बनने वाले महापुरुषों का नामोल्लेख तक कर पाना सम्भव नहीं है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी, 1897 को अवतरित हुए और अपने सम्पूर्ण जीवन की आहुति भारत माता के बन्धन काटने में चढ़ा देने वाले सुभाष बाबू उनमें से एक ऐसे अत्यन्त प्रमुख राजनेता हैं, जो 1916 में प्रेसीडेंसी कालेज, कोलकाता से उस वक्त निष्कासित कर दिए गए थे जब वे बी.ए. के विद्यार्थी थे। वर्ष 1919 में दर्शन शास्त्र विषय में प्रथम श्रेािी में बी.ए. (आनर्स) की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्जित करने के बाद इंग्लैण्ड में मात्र आठ मास के अध्ययन उपरान्त आई.सी.एस. की प्रतियोगात्मक परीक्षा उतीर्ण कर उन्होंने योग्यता सूची में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। किन्तु ब्रिटिश शासन की पराधीनता से घोर वितृष्णा के कारण अप्रैल, 1921 में इंग्लैण्ड में अपने निवास के दौरान ही उससे त्यागपत्र दे दिया। जुलाई, 1921 में भारत आने पर सर्वप्रथम वे गांधी जी से मिले, किन्तु उनसे हुए वार्तालाप से सन्तुष्ट न होने के कारण उन्होंने कलकत्ता जाकर देशबन्धु चित्तरंजनदास से भेंट की और उनके सम्पूर्ण जीवन-काल में वे उनके अत्यंत निष्ठावान अनुयायी बने रहे। महात्मा जी को सुभाष बाबू का यह कार्य रुचिकर नहीं लगा, क्योंकि 1923 में धारा सभाओं अथवा काउंसिल प्रवेश को लेकर इनके देशबन्धु के साथ इतने गम्भीर मतभेद हो गए थे कि 1924 से 1928 के दौरान गांधी जी ने अपने-आपको राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह अलिप्त कर लिया था। सुभाष बाबू को भारतीय राजनीतिक क्षितिज से तिरोहित करने की पराकाष्ठा यद्यपि जनवरी, 1939 में उनके द्वारा डा. पट्टाभि सीतारमैय्या को पराजित करने की घटना से सम्बंधित है, क्योंकि उस समय महात्मा जी और उनके समर्थकों ने मार्च, 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में सुभाष बाबू द्वारा प्रस्तुत छह मास में भारत को स्वाधीनता देने से संबंधित अन्तिमेत्थम्-प्रस्ताव न केवल ठुकरा दिया था, अपितु उसके साथ ही कांग्रेस कार्यसमिति का गठन करना भी असम्भव बना दिया था। दुर्विपाक से कांग्रेस के अन्दर क्रियाशील समाजवादी समूह भी सुभाष बाबू के विरोध में आ डटा था। इसके पूर्व सितम्बर, 1938 में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच हुए कथित म्यूनिख समझौते के तुरन्त बाद जब कांग्रेसाध्यक्ष के रूप में सुभाष बाबू ने सम्पूर्ण देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला संघर्ष करने के उद्देश्य से देशवासियों में बड़े पैमाने पर अपना अभियान आरम्भ किया तब उसका भी खुला विरोध गांधी जी के अनुयायियों द्वारा किया गया, क्योंकि प्रान्तीय स्वायत्तता के अन्तर्गत सत्ता संभालने वाले कांग्रेस के राजनेता अपना मंत्री पद खतरे में डालने को सिद्ध नहीं थे। फलस्वरूप सुभाष बाबू ने 29 अप्रैल, 1939 को कांग्रेसाध्यक्ष पद और कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फारवर्ड ब्लाक नामक संस्था की स्थापना की थी। (देखिए, वही, पृ. 371-373)। इसके पूर्व भी पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को लेकर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के विरुद्ध एक जबरदस्त अभियान चलाया गया था। देश और विदेश में बहुत कम लोगों को इस सच्चाई की जानकारी होगी कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव वर्ष 1929 के अन्त में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व ही पारित किया जा चुका था। तथ्य यह है कि इस घटना के कई वर्ष पूर्व कांग्रेस में बढ़ती हुई युवा शक्ति के जबरदस्त आग्रह पर प्रान्तीय कांग्रेस समितियां पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति से उसे सार्वदेशिक स्तर पर स्वीकार करने का अनुरोध कर रही थीं। फलत: दिसम्बर, 1927 के अन्त में मद्रास में डा. एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में सम्पन्न कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। किन्तु गांधी जी ने अधिवेशन समाप्ति के तुरन्त बाद एक सार्वजनिक वक्तव्य में यह घोषणा की कि उक्त प्रस्ताव 'जल्दबाजी में बिना गम्भीर विचार-विनिमय के पारित किया गया है।' यद्यपि महात्मा जी स्वयं मद्रास कांग्रेस में उपस्थित नहीं थे। तदुपरान्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी सांविधानिक समिति ने बहुमत से कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता के स्थान पर 'डोमिनियन स्टेटसÓ प्राप्त करने की सिफारिश की थी। किन्तु सुभाष बाबू और उनके समर्थकों को वह स्वीकार्य नहीं था। अत: दोनों पक्षों में सहमति बनाने के लिए नवम्बर, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे गांधीजी सहित सुभाष बाबू और दोनों के समर्थकों ने स्वीकार कर लिया। किन्तु दिसम्बर, 1928 में आयोजित कलकत्ता कांग्रेस ने महात्माजी ने मोतीलाल नेहरू के दिल्ली-फार्मूले को मानने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप पूर्ण स्वाधीनता और 'डोमिनियन स्टेटस' के प्रश्न को लेकर अधिवेशन में मतदान हुआ। गांधी जी के समर्थकों द्वारा जोर-शोर से यह प्रचार करने के कारण कि यदि 'डोमीनियन स्टेटस' को अस्वीकृत किया गया तो गांधी जी कांग्रेस की गतिविधियों से अपने आपको सर्वदा के लिए अलग कर लेंगे, मतदान में 'डोमीनियम स्टेटसÓ के पक्ष में 1350 मत और पूर्ण स्वाधीनता के समर्थन में 973 मत आए। (देखिए, वही, पृ. 161-175)। किन्तु इसके एक वर्ष बाद दिसम्बर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वयं गांधी जी ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जोकि मद्रास कांग्रेस की ही भांति सर्वसम्मति से पारित हुआ था। (देखिए, वही, पृ. 192)। सुभाष बाबू के विरुद्ध इससे भी बड़ा गुनाह देश की स्वाधीनता प्राप्ति का श्रेय उन्हें और उनके नेतृत्व में युद्ध-क्षेत्र के अन्दर अद्वितीय वीरता दिखाने वाले आजाद हिन्द फौज के जवानों को न देकर इस मिथ्या-प्रचार को जाता है कि भारत को स्वतंत्रता अहिंसा के मार्ग से गांधी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। इस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रसिद्ध काकोरी काण्ड के एक अप्रतिम स्वतंत्रता सेनानी शचीन्द्रनाथ बख्शी ने वर्ष 1964 में एक लेख के माध्यम से कहा था कि 'अहिंसा से ही मुल्क आजाद हुआ', इस झूठे प्रचार के बाद, आज ऐसा समय आ गया है जब अहिंसा का प्रचार करना देशद्रोह समझा जाने लग गया है।' (देखिए, शचीन्द्रनाथ बख्शी- 'वतन पे मरने वालों का....Ó पृष्ठ 92)। इसी भांति क्रान्तिकारी आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाले मन्मथनाथ गुप्त और सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार ने स्वाधीनता-प्राप्ति का श्रेय नेताजी को दिए जाने की पुष्टि की है। प्रोफेसर मजूमदार ने अंग्रेजी भाषा के अपने ग्रन्थ 'भारत में स्वाधीनता का इतिहास-खण्ड 3 के पृष्ठ 609-610 पर लिखा है कि 1947 में स्वतंत्रता-प्राप्ति में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का योगदान महात्मा गांधी से किसी भी प्रकार कम नहीं था, सम्भवत: वह उससे अधिक महत्वपूर्ण था। ' इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के हैं, जिनके शासन काल में देश स्वतंत्र हुआ। फरवरी, 1947 में ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में भारत को स्वाधीन करने के विषय में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि ब्रिटेन भारतीयों को स्वतंत्रता दे रहा है, क्योंकि अब भारतीय सेना ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति राजभक्त नहीं रही है और ब्रिटेन भारत को अपने अधीन बनाये रखने के लिए अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना को भारत में रखने की स्थिति में नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की इस विवशता की पुष्टि आजाद हिन्द फौज के सेनाधिकारियों के विरुद्ध कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का भारतीय सेनाधिकारियों द्वारा एक स्वर से विरोध करने-जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश राज्य सत्ता को अपनी योजना रद्द करनी पड़ी, 20 जनवरी, 1947 को कराची में भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रारम्भ की गई हड़ताल और उसके लाहौर, मुम्बई और दिल्ली में फैल जाने, 29 फरवरी, 1947 को मुम्बई में नौसेना के 5000 जवानों द्वारा आजाद हिन्द फौज के बिल्ले लगाकर हड़ताल करने तथा कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और कराची के उसकी चपेट में आने की आशंका, मुम्बई में हड़ताली नौसैनिकों द्वारा अंग्रेज सेनाधिकारियों की गोलियों का जवाब सात घंटे तक गोलियों से देने और अन्तत: लार्ड वेवेल द्वारा सरदार पटेल की मध्यस्थता से समझौता करने आदि की घटनाओं से हो जाता है। इतना ही नहीं, बीसवीं शताब्दी में साठ के दशक में जब क्लीमेंट एटली लार्ड के रूप में भारत यात्रा पर आए तब वे कलकत्ता के राजभवन में राज्यपाल के मान्य अतिथि बनकर 3 दिन रुके थे। उस समय राज्यपाल महोदय ने लार्ड एटली से जब यह जानकारी चाही कि 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के पूरी तरह विफल हो जाने और दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन और उसके मित्र-राष्ट्रों को निर्णायक विजय प्राप्त हो जाने पर भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय क्यों लिया? तब इस पर लार्ड एटली का उत्तर था कि इसके अनेक कारण थे जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की भूमिका थी जिसने भारत की थल और नौसेना की ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा के आधार को ही पूरी तरह हिला दिया था। इस पर जब राज्यपाल ने उनसे आगे यह जानकारी प्राप्त करनी चाही कि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन में गांधी जी का कितना योगदान था तब उसे सुनकर एटली के होंठ एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ फैल गए और उन्होंने धीरे-धीरे अपने एक-एक अक्षर पर जोर देते हुए कहा कि न्यूनतम। इससे स्पष्ट है कि भारत को राजनीतिक आजादी प्राप्त कराने में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और उनके नेतृत्व में सक्रिय आजाद हिन्द फौज की निर्णायक भूमिका रही है। इतिहास की इस सच्चाई को उनके 113 वें जन्म दिन के पावन अवसर पर पहचानने की सर्वाधिक आवश्यकता है।
फिर धमाके का दुस्साहस
मुंबई हमलों के बाद शांति थी, लेकिन नए आतंककारी हमले ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। आंतरिक सुरक्षा पर दिल्ली में हाल ही में सम्पन्न मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आतंकवाद व नक्सली आंदोलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग बढाने की जरू रत बताई गई। इससे पहले केन्द्रीय गृहमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कश्मीर के हालात का उल्लेख करते हुए कहा था कि वहां हिंसक घटनाएं कम हुई हैं, हालांकि घुसपैठ बढी है। सम्मेलन में इस बात पर संतोष जताया गया था कि 26/11 के बाद से कोई आतंककारी हमला नहीं हुआ है और सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लश्कर-ए-तैयबा व उसके सहयोगी संगठनों के संभावित आतंककारी हमलों की चेतावनी व संकेतों को ध्यान में रखकर इस पर औपचारिक चर्चा भी होनी चाहिए थी। हाल ही में आजमगढ से पकडे गए शहजाद अहमद से पूछताछ में मिली जानकारी भी स्पष्ट चेतावनी थी। उसने पूछताछ में कहा बताया कि जिन स्थानों पर विदेशी पर्यटकों का आवागमन ज्यादा होता है, वहां इंडियन मुजाहिदीन हमले की साजिश रच रहा है। इन स्थानों में गोवा और आगरा तो थे ही, कई प्रमुख होटल व रेस्टोरेंट भी संभावित लक्ष्यों में शामिल थे, जहां विदेशी पर्यटक अक्सर आते-जाते या ठहरते हैं। इन स्थानों में पुणे की जर्मन बेकरी भी शामिल थी, जिसके पास ही ओशो आश्रम स्थित है। अमरीकी गुप्तचर एजेंसियों ने भी आतंककारियों के ऐसे ही संभावित हमले की सूचना दी थी। अमरीका ने तो भारत आने वाले अमरीकी पर्यटकों को भीडभाड वाले स्थानों से बचने व बेहद सतर्कता बरतने की सलाह भी जारी कर रखी है। इस सबके बावजूद लगता है कि पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती गई। पाकिस्तान आधारित आतंककारी गुटों के निशाने पर पुणे भी है, यह तो लश्कर के डेविड कोलमेन हेडली के दो बार पुणे आने और वहां अब हुए विस्फोट स्थल के पास के एक होटल में ठहरने की जानकारी से ही साफ था। ओशो आश्रम और यहूदियों का उपासना स्थल इस स्थान के निकट होने के कारण वहां विशेष रू प से असाधारण उपाय किए जाने चाहिए थे। अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुए बम विस्फोटों के बाद से ही पुणे को इस्लामी आतंककारी गुटों का एक बडा ठिकाना माना जाता है। तब वहां पुलिस ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुडे आतंककारियों के मददगारों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ में बताया था कि वे कुख्यात आतंककारी तौकीर को जानते हैं, जो पुणे के आजम परिसर में अक्सर आता रहता था। इस परिसर में कई कॉलेज हैं, जिनमें उक्त गिरफ्तार लोगों में से भी कुछ पढते थे। भारतीय गुप्तचर एजेंसियों के पास भी ऐसी सूचनाएं थीं कि भटकल बंधु रियाज व इकबाल और अब्दुस सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर जैसे इंडियन मुजाहिदीन के मुखिया इस इलाके में सक्रिय हैं, हालांकि अब ऐसी सूचनाएं हैं कि ये तीनों अब पाकिस्तान में हैं। निश्चय ही पुणे में इंडियन मुजाहिदीन के ढांचे को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। गुप्तचर एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके मददगार (स्लीपर सैल्स) बचने न पाएं। अहमदाबाद, दिल्ली व जयपुर में हुए बम विस्फोटों और सूरत में बरामद बिना फटे बमों के मामलों की जांच और विस्फोटों से पहले तथा बाद में भेजे गए ई-मेल के आधार पर पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के 21 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे 6 अन्य लोग फरार हैं। इन 21 में से कम से कम 7 या तो पुणे के रहने वाले हैं या वहां से गिरफ्तार हुए हैं। पांच अन्य गिरफ्तार लोग पुणे आ-जा चुके थे और हमलों की साजिश रचने वालों के सहयोगी थे। जांच एजेंसियों ने इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों के खिलाफ जो आरोप तय किए हैं, उनमें पुणे के अशोका म्यूज क्षेत्र में स्थित एक अपार्टमेंट में बम तैयार कर उन्हें लक्ष्य स्थलों तक पहुंचाने का आरोप भी शामिल है। निश्चित रू प से पूरे देश में नहीं, पुणे में भी इंडियन मुजाहिदीन को खत्म करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। सबसे अधिक विक्षुब्ध करने वाला तथ्य यह है कि इतनी सारी जानकारी और गुप्तचर सूचनाओं के बावजूद आतंककारियों के सबसे ज्यादा संभावित हमलों के स्थलों पर सामान्य एहतियाती उपाय तक नहीं किए गए। जनता में जागरूकता की कमी है और जो आम लोग अखबार नहीं पढते या टीवी के न्यूज चैनल नहीं देखते, उन्हें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। यह इस बम विस्फोट का सबसे बडा कारण है। यदि आम आदमी को इस बारे में जागरूक और शिक्षित नहीं किया गया, तो ऐसे बम विस्फोट भविष्य में भी जारी रह सकते हैं। पुणे में इस शनिवार को हुए विस्फोट में वह सुपरिचित तरीका अपनाया गया, जैसा पहले भी कई बम विस्फोटों में अपनाया जा चुका था। लेकिन इस बार विस्फोट के निशाने पर विदेशी पर्यटक थे, इसलिए स्पष्ट है कि इसमें विदेशी हाथ ही होगा। लश्कर-ए-तैयबा भारतीयों का उपयोग कर विश्व को यह बताना चाहता है कि पाकिस्तान या अन्य कोई नहीं स्वयं भारतीय ही विस्फोटों के लिए जिम्मेदार हैं। यह विस्फोट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत फिर शुरू करने की भारत की पेशकश के शीघ्र बाद यह किया गया है। इसका बातचीत पर क्या असर पडेगा, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके बाद भारत वार्ता में निश्चित रूप से अन्य मामलों की तुलना में आतंकवाद को अधिक ध्यान में रखेगा। वार्ता रद्द करना सही कदम नहीं होगा, क्योंकि ?सा करके तो हम आतंककारियों के हाथों में खेलेंगे, जो उपमहाद्वीप में शांति नहीं चाहते। देशवासियों की नजर इस ओर रहेगी कि सरकार विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों को पकडने के लिए क्या कदम उठाती है। सरकार की ओर से सभी प्रयासों के बावजूद आतंककारी कुछ और विस्फोट या हमले करने में सफल हो सकते हैं। जनता को हर कीमत पर विभिन्न समुदायों में शांति सद्भाव कायम रखना चाहिए।
श्रीगुरूजी : एक अनजाना पहलू यह भी
(यह लेख आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक श्रद्धेय श्री सुदर्शनजी द्वारा लिखित है।)
पूजनीय गुरुजी के जून सन् 1973 में दिव्यलोकगमन के पश्चात् उस समय उपलब्ध उनके विचारों के संकलन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हुआ और 'श्री गुरुजी-समग्र दर्शनमाला का भाग-6 सर्वप्रथम मुद्रित हुआ। सन् 1974 के वर्षप्रतिपदा से प्रांत-प्रांतों में उसके विमोचन के कार्यक्रम आयोजित हुए। इंदौर के इस कार्यक्रम में पूजनीय गुरुजी के ज्येष्ठ गुरुभाई स्वामी अमूर्तानन्द जी के सान्निध्य-लाभ का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के उपरांत अनौपचारिक बातचीत में मैंने पूजनीय स्वामीजी से पूछा कि पूजनीय गुरुजी की आध्यात्मिक उपलब्धि क्या थी? पहले तो उन्होंने बताने से मना किया, किन्तु मेरे अधिक आग्रह करने पर कि पूजनीय गुरुजी की अध्यात्म साधाना के आप ही प्रेरक, कारक तथा दर्शक रहे हैं और इसलिए आप नहीं बतायेंगे तो पूजनीय गुरुजी का यह पहलू अनावृत ही रह जाएगा। क्या यह उचित होगा? चिकित्सकों की परेशानी मेरे इस आग्रह के पश्चात् उन्होंने कहा कि पूजनीय गुरुजी ने अपनी आत्मा को शरीर के किसी भाग से अलग कर लेने की क्षमता प्राप्त कर ली थी और इसलिए शरीर के किसी भाग में हुई व्याधि की पीड़ा इच्छा होने पर उन्हें सता नहीं पाती थी। तुरन्त मुझे महर्षि रमण का स्मरण हो आया। महर्षि रमण को भी कर्क-रोग हो गया था और वे तमिलनाडु स्थित अरुणाचलम् से बाहर नहीं जाते थे। अत: चेन्नै शासन ने वहीं अस्थायी शल्यक्रिया कक्ष खड़ा किया व चेन्नै से ख्यातनाम शल्य चिकित्सकों को वहाँ भेजा। जब शल्यक्रिया प्रारंभ करने का समय आया, तब चिकित्सकों ने महर्षि रमण को मूर्च्छावस्था में ले जाना चाहा, जिसे करने से उन्होंने मना कर दिया और बिना संज्ञा-हरक के ही शल्यक्रिया करने के लिए कहा। शल्य चिकित्सक शल्यक्रिया करने में जुट गए, किन्तु उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। जब कर्क रोग की गांठ को काटते हैं, तब तो मृत कोशिकाएँ होती हैं, उन्हें काटने पर तो वेदना नहीं होती, किन्तु जब जीवित कोशिकाओं से शल्य स्पर्श करता है, तब वेदना से मुँह से सिसकारी या चीख निकलती है या मूर्च्छावस्था में शरीर में हलचल होती है जिससे चिकित्सकों को ज्ञात हो जाता है कि वहाँ जीवित कोशिका है। किन्तु महर्षि रमण के मुँह से सिसकारी भी नहीं निकल रही थी। अत: डाक्टरों की परेशानी यह थी कि पता कैसे लगे कि कौन-सी कोशिकाएँ मृत हैं और कौन सी जीवित? असंपृक्त चिकित्सकों ने अपनी परेशानी महर्षि रमण के सामने रखी तो उन्होंने कहा : 'जिस शरीर पर तुम शल्यक्रिया कर रहे हो, वह मैं नहीं हूँ। मैंने अपने आपको शरीर से असंपृक्त कर रखा है और वेदना तो शरीर को होती है।'चिकित्सकों के अनुनय करने पर यह समझौता हुआ कि जब जीवित कोशिकाओं को शल्य स्पर्श करे तो वे अंगुलि उठाकर संकेत कर दें। इस प्रकार करने पर ही शल्यक्रिया पूरी हो सकी थी। दूसरी घटना रामकृष्ण मिशन के स्वामी तुरीयानन्द जी की है। उनकी पीठ में दुष्ट व्रण (कारबंकल) हो गया था और उसकी शल्यक्रिया करने का निश्चय हुआ। दूसरे दिन जब उन्हें मूर्च्छावस्था में ले जाने की तैयारी हुई तब स्वामी जी ने कहा कि मूर्छित किए बिना ही शल्यचिकित्सा करो। सारी क्रिया ठीक तरह से सम्पन्न हुई। दूसरे दिन जब घाव को साफ करने के लिए डाक्टर गए तो पाया कि एक छोटा-सा टुकड़ा बच गया है। उन्होंने सोचा कि निकाल दें। पर ज्यों ही निकाला तो स्वामी जी के मुंह से जोर की चीख निकली। डाक्टर हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा : 'स्वामी जी कल सारा व्रण निकाला, तब तो आप शान्त रहे, आज छोटा-सा बचा टुकड़ा निकालने पर चीख क्यों पड़े?Óतब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि 'पहले बताते तो मैं अपने-आप को शरीर के उस भाग से समेट लेता। कल मैंने वैसा ही किया था इसलिए वेदना नहीं हुई।'डा. परांजपे की भूल पूजनीय गुरुजी के कर्क की गठान पर जब शल्यक्रिया हुई तब उन्हें मूर्चि्छत तो अवश्य किया गया, किन्तु जैसे ही संज्ञा-हरक का प्रभाव समाप्त होकर वे होश में आए, त्यों ही कमरे से बाहर निकलकर आस-पास के कमरों में जाकर रोगियों का हालचाल पूछने लगे। शल्यचिकित्सा के पश्चात् पूजनीय गुरुजी ने नागपुर में मा. बाबासाहब घटाटे के यहाँ कुछ दिन विश्राम किया, जहाँ घाव की साफ-सफाई करने के लिए डा. रामदास परांजपे रोज जाया करते थे। डा. परांजपे साफ-सफाई करते और उधर पूजनीय गुरुजी के मुँह से हास्यविनोद की फुलझडिय़ाँ झड़तीं और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण बन जाता। एक दिन डा. परांजपे के हाथ से अनजाने में एक भूल हो गई। रक्त से सने कपास के टुकड़े को निकालते समय उस टुकड़े के स्थान पर मांस का खंड चिमटी की पकड़ में आ गया और रक्त बह चला। यह देखकर सभी के मुँह से सीत्कार फूट पड़ा। डा. परांजपे का मन भी ग्लानि से भर गया और वे अपनी प्रमाद के लिए पूजनीय गुरुजी से क्षमायाचना करने लगे। असहनीय पीड़ा में भी प्रफुल्लता डा. परांजपे की भावनाओं को सहलाते हुए श्री गुरुजी ने बड़े शांत चित्त से उत्तर दिया : 'आप व्यर्थ ही मन में कष्ट मान रहे हैं। कपास के टुकड़े और मांस में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए दोनों समान हैं। जब आप घाव को साफ करते हैं, तब तक मेरा मन शरीर से अलग रहता है और जब मन शरीर से अलग रहता है तब शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं होता। 'डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर लिखते हैं : 'यह सब जानते हैं कि कर्करोग की शल्यक्रिया के बाद भी गुरुजी के शरीर में बहुत जलन रहा करती थी और कष्ट भी अपार था, पर उनसे बात करते समय कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता था कि उन्हें इतनी अधिक पीड़ा है। प्रफुल्ल मुखाकृति की छाप लेकर ही गुरुजी के पास से लोग लौटा करते। 'आगे चलकर अकड़ी बाँह की अग्निदग्धा चिकित्सा पुणे में कराई गई। उसे कराते समय उन्होंने संज्ञा-शून्य करने से मना कर दिया। जब अग्नि से दाग दिया जाता था तब मांस जलने की 'चर्रर्' की आवाज आती थी, पूजनीय गुरुजी के निजी सचिव डा. आबाजी थत्ते तक उस दृश्य को देख नहीं सके और कमरे से बाहर चले गए, किन्तु पूजनीय गुरुजी ने शांतचित्त से सब सहा। रोग का कारण पूजनीय गुरुजी को कर्करोग होने का क्या कारण रहा होगा? इस संबंध में पूजनीय गुरुजी के साथ एक वार्तालाप का स्मरण होता है। अनौपचारिक बातचीत में उनसे प्राणायाम के संबंध में चर्चा चल पड़ी। उन्होंने बताया कि 'प्राणायाम किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। प्राणायाम की क्रिया में पूरक (श्वास अंदर लेना) और रेचक (श्वास बाहर छोडऩा) तो विशेष हानिकारक नहीं हैं किन्तु कुंभक (श्वास रोके रखना) अतीव सावधानी की अपेक्षा रखता है। ठीक विधि से प्राणायाम क्रिया करने पर प्राण नियंत्रित होता है, किन्तु यदि उसमें गड़बड़ हुई तो प्राण नियंत्रित होने के स्थान पर कुपित हो सकता है।Óऔर यह कहते हुए उन्होंने अपने खुद का अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा : 'मैं रोज संध्या करते समय प्राणायाम भी किया करता था। एक दिन कक्ष का द्वार केवल भिड़ा हुआ था। मैं जब कुंभक की स्थिति में था तब शरीर किसी भी प्रकार का धक्का सहन करने की स्थिति में नहीं था। उसी समय मेरी चार वर्ष की नातिन अंदर आई और मेरी पीठ पर लद गई। उसके कारण छाती में बायीं ओर जो दर्द शुरू हुआ वह आज तक नहीं गया।Óआगे चलकर हमने देखा कि उसी स्थान पर कर्क की गठान उभरी। साक्षात्कार पूजनीय गुरुजी को साक्षात्कार हुआ था या नहीं, इस संबंधा में महाराष्ट्र के एक संत श्री दत्ता बाळ ने श्रध्दांजलि सभा में कहा था : 'मेरे व्याख्यानों का कार्यक्रम जब नागपुर में आयोजित हुआ, तब मैंने देखा कि एक दाढ़ी-मूँछ व लंबे केशवाले सज्जन कार्यक्रम में आए हैं। मैंने अपने साथियों से पूछा कि वे कौन हैं? तब बताया गया कि वे गुरुजी गोलवलकर हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति कोई आदर का भाव नहीं था। किन्तु उन्हें अपने कार्यक्रम में देखकर मुझे कौतूहल हुआ और दूसरे दिन उनसे मिलने डा. हेडगेवार भवन चला गया। उनसे एकांत में वार्तालाप में मैंने योग संबंधी कुछ प्रश्न पूछे। मैंने अनुभव किया कि वे जो उत्तर देते थे, वे एक स्तर से आगे के रहते थे। इस प्रकार एक-एक सीढ़ी हम ऊपर उठते गए। अंत में मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया : 'गुरुजी, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए हैं?'उन्होंने मेरी ओर कुछ देर तक देखा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि 'एक शर्त पर ही बताता हूँ कि किसी से कहोगे नहीं।Óमेरे हाँ कहने पर उन्होंने कहा : ''हाँ, हुआ है। संघ पर लगे प्रतिबंध के समय जब मैं सिवनी जेल में था और खाट पर बैठे हुए सारे घटनाक्रम के बारे में चिंतित हो रहा था, तब मुझे लगा कि कोई मेरे कंधो को दबा रहा है। जब पलटकर ऊपर देखा तो साक्षात् जगज्जननी-माँ सामने खड़ी थी। उसने आश्वस्त करते हुए कहा - 'सब ठीक होगा।'उसी बलबूते पर तो आगे के सारे संकटों का मैं दृढ़ता के साथ सामना कर सका।'और यह सुनाते हुए श्री दत्ता बाळ ने कहा : 'चूंकि अब वे दिवंगत हो गए हैं, इसलिए उनको दिए गए अभिवचन से मैं मुक्त हो गया हूँ और यह बात आप सबको बता रहा हूँ। ऐसे एक अध्यात्म-शक्तिसम्पन्न व्यक्ति के दर्शन, निर्देशन, सान्निध्य और नेतृत्व का लाभ हम सबको मिल सका, इसे अपने पूर्वजन्मों के सुकृत का ही परिणाम मानना होगा।
पूजनीय गुरुजी के जून सन् 1973 में दिव्यलोकगमन के पश्चात् उस समय उपलब्ध उनके विचारों के संकलन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हुआ और 'श्री गुरुजी-समग्र दर्शनमाला का भाग-6 सर्वप्रथम मुद्रित हुआ। सन् 1974 के वर्षप्रतिपदा से प्रांत-प्रांतों में उसके विमोचन के कार्यक्रम आयोजित हुए। इंदौर के इस कार्यक्रम में पूजनीय गुरुजी के ज्येष्ठ गुरुभाई स्वामी अमूर्तानन्द जी के सान्निध्य-लाभ का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के उपरांत अनौपचारिक बातचीत में मैंने पूजनीय स्वामीजी से पूछा कि पूजनीय गुरुजी की आध्यात्मिक उपलब्धि क्या थी? पहले तो उन्होंने बताने से मना किया, किन्तु मेरे अधिक आग्रह करने पर कि पूजनीय गुरुजी की अध्यात्म साधाना के आप ही प्रेरक, कारक तथा दर्शक रहे हैं और इसलिए आप नहीं बतायेंगे तो पूजनीय गुरुजी का यह पहलू अनावृत ही रह जाएगा। क्या यह उचित होगा? चिकित्सकों की परेशानी मेरे इस आग्रह के पश्चात् उन्होंने कहा कि पूजनीय गुरुजी ने अपनी आत्मा को शरीर के किसी भाग से अलग कर लेने की क्षमता प्राप्त कर ली थी और इसलिए शरीर के किसी भाग में हुई व्याधि की पीड़ा इच्छा होने पर उन्हें सता नहीं पाती थी। तुरन्त मुझे महर्षि रमण का स्मरण हो आया। महर्षि रमण को भी कर्क-रोग हो गया था और वे तमिलनाडु स्थित अरुणाचलम् से बाहर नहीं जाते थे। अत: चेन्नै शासन ने वहीं अस्थायी शल्यक्रिया कक्ष खड़ा किया व चेन्नै से ख्यातनाम शल्य चिकित्सकों को वहाँ भेजा। जब शल्यक्रिया प्रारंभ करने का समय आया, तब चिकित्सकों ने महर्षि रमण को मूर्च्छावस्था में ले जाना चाहा, जिसे करने से उन्होंने मना कर दिया और बिना संज्ञा-हरक के ही शल्यक्रिया करने के लिए कहा। शल्य चिकित्सक शल्यक्रिया करने में जुट गए, किन्तु उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। जब कर्क रोग की गांठ को काटते हैं, तब तो मृत कोशिकाएँ होती हैं, उन्हें काटने पर तो वेदना नहीं होती, किन्तु जब जीवित कोशिकाओं से शल्य स्पर्श करता है, तब वेदना से मुँह से सिसकारी या चीख निकलती है या मूर्च्छावस्था में शरीर में हलचल होती है जिससे चिकित्सकों को ज्ञात हो जाता है कि वहाँ जीवित कोशिका है। किन्तु महर्षि रमण के मुँह से सिसकारी भी नहीं निकल रही थी। अत: डाक्टरों की परेशानी यह थी कि पता कैसे लगे कि कौन-सी कोशिकाएँ मृत हैं और कौन सी जीवित? असंपृक्त चिकित्सकों ने अपनी परेशानी महर्षि रमण के सामने रखी तो उन्होंने कहा : 'जिस शरीर पर तुम शल्यक्रिया कर रहे हो, वह मैं नहीं हूँ। मैंने अपने आपको शरीर से असंपृक्त कर रखा है और वेदना तो शरीर को होती है।'चिकित्सकों के अनुनय करने पर यह समझौता हुआ कि जब जीवित कोशिकाओं को शल्य स्पर्श करे तो वे अंगुलि उठाकर संकेत कर दें। इस प्रकार करने पर ही शल्यक्रिया पूरी हो सकी थी। दूसरी घटना रामकृष्ण मिशन के स्वामी तुरीयानन्द जी की है। उनकी पीठ में दुष्ट व्रण (कारबंकल) हो गया था और उसकी शल्यक्रिया करने का निश्चय हुआ। दूसरे दिन जब उन्हें मूर्च्छावस्था में ले जाने की तैयारी हुई तब स्वामी जी ने कहा कि मूर्छित किए बिना ही शल्यचिकित्सा करो। सारी क्रिया ठीक तरह से सम्पन्न हुई। दूसरे दिन जब घाव को साफ करने के लिए डाक्टर गए तो पाया कि एक छोटा-सा टुकड़ा बच गया है। उन्होंने सोचा कि निकाल दें। पर ज्यों ही निकाला तो स्वामी जी के मुंह से जोर की चीख निकली। डाक्टर हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा : 'स्वामी जी कल सारा व्रण निकाला, तब तो आप शान्त रहे, आज छोटा-सा बचा टुकड़ा निकालने पर चीख क्यों पड़े?Óतब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि 'पहले बताते तो मैं अपने-आप को शरीर के उस भाग से समेट लेता। कल मैंने वैसा ही किया था इसलिए वेदना नहीं हुई।'डा. परांजपे की भूल पूजनीय गुरुजी के कर्क की गठान पर जब शल्यक्रिया हुई तब उन्हें मूर्चि्छत तो अवश्य किया गया, किन्तु जैसे ही संज्ञा-हरक का प्रभाव समाप्त होकर वे होश में आए, त्यों ही कमरे से बाहर निकलकर आस-पास के कमरों में जाकर रोगियों का हालचाल पूछने लगे। शल्यचिकित्सा के पश्चात् पूजनीय गुरुजी ने नागपुर में मा. बाबासाहब घटाटे के यहाँ कुछ दिन विश्राम किया, जहाँ घाव की साफ-सफाई करने के लिए डा. रामदास परांजपे रोज जाया करते थे। डा. परांजपे साफ-सफाई करते और उधर पूजनीय गुरुजी के मुँह से हास्यविनोद की फुलझडिय़ाँ झड़तीं और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण बन जाता। एक दिन डा. परांजपे के हाथ से अनजाने में एक भूल हो गई। रक्त से सने कपास के टुकड़े को निकालते समय उस टुकड़े के स्थान पर मांस का खंड चिमटी की पकड़ में आ गया और रक्त बह चला। यह देखकर सभी के मुँह से सीत्कार फूट पड़ा। डा. परांजपे का मन भी ग्लानि से भर गया और वे अपनी प्रमाद के लिए पूजनीय गुरुजी से क्षमायाचना करने लगे। असहनीय पीड़ा में भी प्रफुल्लता डा. परांजपे की भावनाओं को सहलाते हुए श्री गुरुजी ने बड़े शांत चित्त से उत्तर दिया : 'आप व्यर्थ ही मन में कष्ट मान रहे हैं। कपास के टुकड़े और मांस में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए दोनों समान हैं। जब आप घाव को साफ करते हैं, तब तक मेरा मन शरीर से अलग रहता है और जब मन शरीर से अलग रहता है तब शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं होता। 'डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर लिखते हैं : 'यह सब जानते हैं कि कर्करोग की शल्यक्रिया के बाद भी गुरुजी के शरीर में बहुत जलन रहा करती थी और कष्ट भी अपार था, पर उनसे बात करते समय कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता था कि उन्हें इतनी अधिक पीड़ा है। प्रफुल्ल मुखाकृति की छाप लेकर ही गुरुजी के पास से लोग लौटा करते। 'आगे चलकर अकड़ी बाँह की अग्निदग्धा चिकित्सा पुणे में कराई गई। उसे कराते समय उन्होंने संज्ञा-शून्य करने से मना कर दिया। जब अग्नि से दाग दिया जाता था तब मांस जलने की 'चर्रर्' की आवाज आती थी, पूजनीय गुरुजी के निजी सचिव डा. आबाजी थत्ते तक उस दृश्य को देख नहीं सके और कमरे से बाहर चले गए, किन्तु पूजनीय गुरुजी ने शांतचित्त से सब सहा। रोग का कारण पूजनीय गुरुजी को कर्करोग होने का क्या कारण रहा होगा? इस संबंध में पूजनीय गुरुजी के साथ एक वार्तालाप का स्मरण होता है। अनौपचारिक बातचीत में उनसे प्राणायाम के संबंध में चर्चा चल पड़ी। उन्होंने बताया कि 'प्राणायाम किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। प्राणायाम की क्रिया में पूरक (श्वास अंदर लेना) और रेचक (श्वास बाहर छोडऩा) तो विशेष हानिकारक नहीं हैं किन्तु कुंभक (श्वास रोके रखना) अतीव सावधानी की अपेक्षा रखता है। ठीक विधि से प्राणायाम क्रिया करने पर प्राण नियंत्रित होता है, किन्तु यदि उसमें गड़बड़ हुई तो प्राण नियंत्रित होने के स्थान पर कुपित हो सकता है।Óऔर यह कहते हुए उन्होंने अपने खुद का अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा : 'मैं रोज संध्या करते समय प्राणायाम भी किया करता था। एक दिन कक्ष का द्वार केवल भिड़ा हुआ था। मैं जब कुंभक की स्थिति में था तब शरीर किसी भी प्रकार का धक्का सहन करने की स्थिति में नहीं था। उसी समय मेरी चार वर्ष की नातिन अंदर आई और मेरी पीठ पर लद गई। उसके कारण छाती में बायीं ओर जो दर्द शुरू हुआ वह आज तक नहीं गया।Óआगे चलकर हमने देखा कि उसी स्थान पर कर्क की गठान उभरी। साक्षात्कार पूजनीय गुरुजी को साक्षात्कार हुआ था या नहीं, इस संबंधा में महाराष्ट्र के एक संत श्री दत्ता बाळ ने श्रध्दांजलि सभा में कहा था : 'मेरे व्याख्यानों का कार्यक्रम जब नागपुर में आयोजित हुआ, तब मैंने देखा कि एक दाढ़ी-मूँछ व लंबे केशवाले सज्जन कार्यक्रम में आए हैं। मैंने अपने साथियों से पूछा कि वे कौन हैं? तब बताया गया कि वे गुरुजी गोलवलकर हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति कोई आदर का भाव नहीं था। किन्तु उन्हें अपने कार्यक्रम में देखकर मुझे कौतूहल हुआ और दूसरे दिन उनसे मिलने डा. हेडगेवार भवन चला गया। उनसे एकांत में वार्तालाप में मैंने योग संबंधी कुछ प्रश्न पूछे। मैंने अनुभव किया कि वे जो उत्तर देते थे, वे एक स्तर से आगे के रहते थे। इस प्रकार एक-एक सीढ़ी हम ऊपर उठते गए। अंत में मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया : 'गुरुजी, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए हैं?'उन्होंने मेरी ओर कुछ देर तक देखा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि 'एक शर्त पर ही बताता हूँ कि किसी से कहोगे नहीं।Óमेरे हाँ कहने पर उन्होंने कहा : ''हाँ, हुआ है। संघ पर लगे प्रतिबंध के समय जब मैं सिवनी जेल में था और खाट पर बैठे हुए सारे घटनाक्रम के बारे में चिंतित हो रहा था, तब मुझे लगा कि कोई मेरे कंधो को दबा रहा है। जब पलटकर ऊपर देखा तो साक्षात् जगज्जननी-माँ सामने खड़ी थी। उसने आश्वस्त करते हुए कहा - 'सब ठीक होगा।'उसी बलबूते पर तो आगे के सारे संकटों का मैं दृढ़ता के साथ सामना कर सका।'और यह सुनाते हुए श्री दत्ता बाळ ने कहा : 'चूंकि अब वे दिवंगत हो गए हैं, इसलिए उनको दिए गए अभिवचन से मैं मुक्त हो गया हूँ और यह बात आप सबको बता रहा हूँ। ऐसे एक अध्यात्म-शक्तिसम्पन्न व्यक्ति के दर्शन, निर्देशन, सान्निध्य और नेतृत्व का लाभ हम सबको मिल सका, इसे अपने पूर्वजन्मों के सुकृत का ही परिणाम मानना होगा।
छत्रपति शिवाजी के पथ प्रदर्शक : समर्थ रामदास
समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरू थे। उन्होने दासबोध नामक एक ग्रन्थ की रचना की जो मराठी में है।
जीवन चरित :- समर्थ रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजीपंत कुलकर्णी (ठोसर) था। इनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जांब नामक स्थान पर शके 1530 में हुआ। वे बचपन में बहुत शरारती थे। गाँव के लोग रोज उनकी शिकायत उनकी माता से करते थे। एक दिन माता राणुबाई ने नारायण (यह उनके बचपन का नाम था) से कहा, 'तुम दिनभर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं!' यह बात नारायण के मन में घर कर गई। दो-तीन दिन बाद यह बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यानमग्न बैठ गया। दिनभर में नारायण नहीं दिखा तो माता ने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ है।उसने भी कहा, 'मैंने उसे नहीं देखा।' दोनों को चिंता हुई और उन्हें ढूँढने निकले पर, उनका कोई पता नहीं चला। शाम के वक्त माता ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, 'नारायण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?' तब नारायण ने जवाब दिया, 'मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा 'इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या बदल गई। उन्होंने समाज के युवा वर्ग को यह समझाया कि स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसलिए उन्होंने व्यायाम एवं कसरत करने की सलाह दी एवं शक्ति के उपासक हनुमानजी की मूर्ति की स्थापना की। समस्त भारत का उन्होंने पद-भ्रमण किया।
जगह-जगह पर हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की, जगह-जगह मठ एवं मठाधीश बनाए ताकि पूरे राष्ट्र में नव-चेतना का निर्माण हो। आख्यायिका है कि 12 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह के समय 'शुभमंगल सावधान' में 'सावधान' शब्द सुनकर वे विवाहमंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्रीरामचंद्र की उपासना में संलग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष तक वे लीन रहे। यहीं उनका नाम 'रामदास' पड़ा। इसके बाद 12 वर्ष तक वे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। इस प्रवस में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्षसाधना के स्थान पर अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना द्वारा आततायी शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। शासन के विरुद्ध जनता को संघटित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्यस्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति श्रीशिवाजी महाराज जैसे योग्य शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज्यस्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवनकाल में ही प्राप्त हो सका। उन्होंने शके 1603 में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ली।
प्रभु दर्शन :-
बचपन में ही उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्रजी के दर्शन हुए थे। इसलिए वे अपने आपको रामदास कहलाते थे। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। शिवाजी महाराज रामदासजी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा जब इनका मिलन हुआ तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदासजी की झोली में डाल दिया। रामदासजी ने महाराज से कहा, 'यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा। यह राज्य भगवान का है, हम सिर्फ न्यासी हैं।' शिवाजी समय-समय पर उनसे सलाह-मशविरा किया करते थे। रामदास स्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे। इसमें 'दासबोध' प्रमुख है। इसी प्रकार उन्होंने हमारे मन को भी संस्कारित किया 'मनाचे श्लोक' द्वारा।
अंतिम समय :-
अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने सातारा के पास परळी के किले पर व्यतीत किया। इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ा। वहीं उनकी समाधि स्थित है। यहाँ पर दास नवमी पर 2 से 3 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष समर्थ रामदास स्वामी के भक्त भारत के विभिन्न प्रांतों में 2 माह का दौरा निकालते हैं और दौरे में मिली भिक्षा से सज्जनगढ़ की व्यवस्था चलती है।
जीवन चरित :- समर्थ रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजीपंत कुलकर्णी (ठोसर) था। इनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जांब नामक स्थान पर शके 1530 में हुआ। वे बचपन में बहुत शरारती थे। गाँव के लोग रोज उनकी शिकायत उनकी माता से करते थे। एक दिन माता राणुबाई ने नारायण (यह उनके बचपन का नाम था) से कहा, 'तुम दिनभर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं!' यह बात नारायण के मन में घर कर गई। दो-तीन दिन बाद यह बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यानमग्न बैठ गया। दिनभर में नारायण नहीं दिखा तो माता ने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ है।उसने भी कहा, 'मैंने उसे नहीं देखा।' दोनों को चिंता हुई और उन्हें ढूँढने निकले पर, उनका कोई पता नहीं चला। शाम के वक्त माता ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, 'नारायण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?' तब नारायण ने जवाब दिया, 'मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा 'इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या बदल गई। उन्होंने समाज के युवा वर्ग को यह समझाया कि स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसलिए उन्होंने व्यायाम एवं कसरत करने की सलाह दी एवं शक्ति के उपासक हनुमानजी की मूर्ति की स्थापना की। समस्त भारत का उन्होंने पद-भ्रमण किया।
जगह-जगह पर हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की, जगह-जगह मठ एवं मठाधीश बनाए ताकि पूरे राष्ट्र में नव-चेतना का निर्माण हो। आख्यायिका है कि 12 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह के समय 'शुभमंगल सावधान' में 'सावधान' शब्द सुनकर वे विवाहमंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्रीरामचंद्र की उपासना में संलग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष तक वे लीन रहे। यहीं उनका नाम 'रामदास' पड़ा। इसके बाद 12 वर्ष तक वे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। इस प्रवस में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्षसाधना के स्थान पर अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना द्वारा आततायी शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। शासन के विरुद्ध जनता को संघटित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्यस्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति श्रीशिवाजी महाराज जैसे योग्य शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज्यस्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवनकाल में ही प्राप्त हो सका। उन्होंने शके 1603 में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ली।
प्रभु दर्शन :-
बचपन में ही उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्रजी के दर्शन हुए थे। इसलिए वे अपने आपको रामदास कहलाते थे। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। शिवाजी महाराज रामदासजी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा जब इनका मिलन हुआ तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदासजी की झोली में डाल दिया। रामदासजी ने महाराज से कहा, 'यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा। यह राज्य भगवान का है, हम सिर्फ न्यासी हैं।' शिवाजी समय-समय पर उनसे सलाह-मशविरा किया करते थे। रामदास स्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे। इसमें 'दासबोध' प्रमुख है। इसी प्रकार उन्होंने हमारे मन को भी संस्कारित किया 'मनाचे श्लोक' द्वारा।
अंतिम समय :-
अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने सातारा के पास परळी के किले पर व्यतीत किया। इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ा। वहीं उनकी समाधि स्थित है। यहाँ पर दास नवमी पर 2 से 3 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष समर्थ रामदास स्वामी के भक्त भारत के विभिन्न प्रांतों में 2 माह का दौरा निकालते हैं और दौरे में मिली भिक्षा से सज्जनगढ़ की व्यवस्था चलती है।
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय
भारत की आजादी के आन्दोलन के प्रखर नेता लाला लाजपथ राय का नाम ही देशवासियों में स्फूर्ति तथा प्रेरणा का संचार कराता है। अपने देश धर्म तथा संस्कृति के लिए उनमें जो प्रबल प्रेम तथा आदर था उसी के कारण वे स्वयं को राष्ट्र के लिए समर्पित कर अपना जीवन दे सके। भारत को स्वाधीनता दिलाने में उनका त्याग, बलिदान तथा देशभक्ति अद्वितीय और अनुपम थी। उनके बहुविधि क्रियाकलाप में साहित्य-लेखन एक महत्वपूर्ण आयाम है। वे ऊर्दू तथा अंग्रेजी के समर्थ रचनाकार थे। लालाजी का जन्म 28 जनवरी, 1865 को अपने ननिहाल के गाँव ढुंढिके (जिला फरीदकोट, पंजाब) में हुआ था। उनके पिता लाला राधाकृष्ण लुधियाना जिले के जगराँव कस्बे के निवासी अग्रवाल वैश्य थे। लाला राधाकृष्ण अध्यापक थे। लाजपतराय की शिक्षा पाँचवें वर्ष में आरम्भ हुई। 1880 में उन्होंने कलकत्ता तथा पंजाब विश्वविद्यायल से एंट्रेंस की परीक्षा एक वर्ष में पास की और आगे पढऩे के लिए लाहौर आये। यहाँ वे गर्वमेंट कालेज में प्रविष्ट हुए और 1982 में एफ0 ए0 की परीक्षा तथा मुख्यारी की परीक्षा साथ-साथ पास की। यहीं वे आर्यसमाज के सम्पर्क में आये और उसके सदस्य बन गये। लाला साँईदास आर्यसमाज के प्रति इतने अधिक समर्पित थे कि वे होनहार नवयुवकों को इस संस्था में प्रविष्ट करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। स्वामी श्रद्धानन्द (तत्कालीन लाला मुंशीराम) को आर्यसमाज में लाने का श्रेय भी उन्हें ही है। 30 अक्टूबर, 1883 को जब अजमेर में ऋषि दयानन्द का देहान्त हो गया तो 9 नवम्बर, 1883 को लाहौर आर्यसमाज की ओर एक शोकसभा का आयोजन किया गया। इस सभा के अन्त में यह निश्चित हुआ कि स्वामी जी की स्मृति में एक ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की जाये जिसमें वैदिक साहित्य, संस्कृति तथा हिन्दी की उच्च शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान -विज्ञान में भी छात्रों को दक्षता प्राप्त कराई जाये। 1886 में जब इस शिक्षण की स्थापना हुई तो आर्यसमाज के अन्य नेताओं के साथ लाला लाजपतराय का भी इसके संचालन में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा तथा वे कालान्तर में डी0ए0वी0 कालेज, लाहौर के महान स्तम्भ बने।
वकालत के क्षेत्र में :- लाला लाजपतराय ने एक मुख्तार (छोटा वकील) के रूप में अपने मूल निवासस्थल जगराँव में ही वकालत आरम्भ कर दी थी; किन्तु यह कस्बा बहुत छोटा था, जहाँ उनके कार्य के बढऩे की अधिक सम्भावना नहीं थी, अत: वे रोहतक चले गये। रोहतक में 1885 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, 1886 में वे हिसार आ गये। एक सफल वकील के रूप में 1892 तक वे यहीं रहे और इसी वर्ष लाहौर आये। तब से लाहौर ही उनकी सार्वजनिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया। लालाजी ने अपने साथियों सहित सामाजिक हित की योजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान किया किन्तु लाहौर आने पर वे आर्यसमाज के अतिरिक्त राजनैतिक आन्दोलन के साथ भी जुड़ गये। 1888 में वे प्रथम बार कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में सम्मिलित हुए जिनकी अध्यक्षता मि0 जार्ज यूल ने की थी। 1906 में वे प0 गोपालकृष्ण गोखले के साथ कांग्रेस के एक शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में इंग्लैड गये। यहाँ से वे अमेरिका चले गये। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएँ की और वहाँ रहकर पश्चिमी देशों के समक्ष भारत की राजनैतिक परिस्थिति की वास्तविकता से वहां के लोगों को परिचित कराया तथा उन्हें स्वाधीनता आन्दोलन की जानकारी दी। लाला लाजपतराय ने अपने सहयोगियों-लोकमान्य तिलक तथा विपिनचन्द्र पाल के साथ मिलकर कांग्रेस में उग्र विचारों का प्रवेश कराया। 1885 में अपनी स्थापना से लेकर लगभग बीस वर्षो तक कांग्रेस ने एक राजभवन संस्था का चरित्र बनाये रखा था। इसके नेतागण वर्ष में एक बार बड़े दिन की छुट्टियों में देश के किसी नगर में एकत्रित होने और विनम्रता पूर्वक शासनों के सूत्रधारों (अंग्रेजी) से सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को अधिकाधिक संख्या में प्रविष्ट युगराज के भारत-आगमन पर उनका स्वागत करने का प्रस्ताव आया तो लालाजी ने उनका डटकर विरोध किया। कांग्रेस के मंच ये यह अपनी किस्म का पहला तेजस्वी भाषण हुआ जिसमें देश की अस्मिता प्रकट हुई थी। 1907 में जब पंजाब के किसानों में अपने अधिकारों को लेकर चेतना उत्पन्न हुई तो सरकार का क्रोध लालाजी तथा सरदार अजीतसिंह (शहीद भगतसिंह के चाचा) पर उमड़ पड़ा और इन दोनों देशभक्त नेताओं को देश से निर्वासित कर उन्हें पड़ोसी देश बर्मा के मांडले नगर में नजरबंद कर दिया, किन्तु देशवासियों द्वारा सरकार के इस दमनपूर्ण कार्य का प्रबल विरोध किये जाने पर सरकार को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा। लालाजी पुन: स्वदेश आये और देशवासियों ने उनका भावभीना स्वागत किया। लालाजी के राजनैतिक जीवन की कहानी अत्यन्त रोमांचक तो है ही, भारतीयों को स्वदेश-हित के लिए बलिदान तथा महान् त्याग करने की प्रेरणा भी देती है।
जन-सेवा के कार्य :- लालाजी केवल राजनैतिक नेता और कार्यकर्ता ही नहीं थे। उन्होंने जन सेवा का भी सच्चा पाठ पढ़ा था। जब 1896 तथा 1899 (इसे राजस्थान में छप्पन का अकाल कहते हैं, क्योंकि यह विक्रम का 1956 का वर्ष था) में उत्तर भारत में भयंकर दुष्काल पड़ा तो लालाजी ने अपने साथी लाला हंसराज के सहयोग से अकालपीडि़त लोगों को सहायता पहुँचाई। जिन अनाथ बच्चों को ईसाई पादरी अपनाने के लिए तैयार थे और अन्तत: जो उनका धर्म-परिवर्तन करने के इरादे रखते थे उन्हें इन मिशनरियों के चुंगुल से बचाकर फीरोजपुर तथा आगरा के आर्य अनाथलायों में भेजा। 1905 में कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में भयंकर भूकम्प आया। उस समय भी लालाजी सेवा-कार्य में जुट गये और डी0ए0वी0 कालेज लाहौर के छात्रों के साथ भूकम्प-पीडि़तों को राहत प्रदान की।
1907-08 में उड़ीसा मध्यप्रदेश तथा संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) से भी भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा और लालाजी को पीडितों की सहायता के लिए आगे आना पड़ा। पुन: राजनैतिक आन्दोलन में 1907 के सूरत के प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपतराय ने अपने सहयोगियों के द्वारा राजनीति में गरम दल की विचारधारा का सूत्रपात कर दिया था और जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गये थे कि केवल प्रस्ताव पास करने और गिड़गिड़ाने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। हम यह देख चुके हैं कि जनभावना को देखते हुए अंग्रेजों को उनके देश-निर्वासन को रद्द करना पड़ा था। वे स्वदेश आये और पुन: स्वाधीनता के संघर्ष में जुट गये। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) के दौरान वे एक प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में पुन: इंग्लैंड गये और देश की आजादी के लिए प्रबल जनमत जागृत किया। वहाँ से वे जापान होते हुए अमेरिका चले गये और स्वाधीनता-प्रेमी अमेरिकावासियों के समक्ष भारत की स्वाधीनता का पथ प्रबलता से प्रस्तुत किया। यहाँ इण्डियन होम रूल लीग की स्थापना की तथा कुछ ग्रन्थ भी लिखे। 20 फरवरी, 1920 को जब वे स्वदेश लौटे तो अमृतसर में जलियावाला बाग काण्ड हो चुका था और सारा राष्ट्र असन्तोष तथा क्षोभ की ज्वाला में जल रहा था। इसी बीच महात्मा गांधी ने सहयोग आन्दोलन आरम्भ किया तो लालाजी पूर्ण तत्परता के साथ इस संघर्ष में जुट गये। 1920 में ही वे कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। उन दिनों सरकारी शिक्षण संस्थानों के बहिस्कार विदेशी वस्त्रों के त्याग, अदालतों का बहिष्कार, शराब के विरुद्ध आन्दोलन, चरखा और खादी का प्रचार जैसे कार्यक्रमों को कांग्रेस ने अपने हाथ में ले रखा था, जिसके कारण जनता में एक नई चेतना का प्रादुर्भाव हो चला था। इसी समय लालाजी को कारावास का दण्ड मिला, किन्तु खराब स्वास्थ्य के कारण वे जल्दी ही रिहा कर दिये गये। 1924 में लालाजी कांग्रेस के अन्तर्गत ही बनी स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गये और केन्द्रीय धारा सभा (सेंटल असेम्बली) के सदस्य चुन लिए गये। जब उनका पं0 मोतीलाल नेहरू से कतिपय राजनैतिक प्रश्नों पर मतभेद हो गया तो उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया और पुन: असेम्बली में पहुँच गये। अन्य विचारशील नेताओं की भाँति लालाजी भी कांग्रेस में दिन-प्रतिदिन बढऩे वाली मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से अप्रसन्नता अनुभव करते थे, इसलिए स्वामी श्रद्धानन्द तथा पं0 मदनमोहन मालवीय के सहयोग से उन्होंने हिन्दू महासभा के कार्य को आगे बढ़ाया। 1925 में उन्हें हिन्दू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। ध्यातव्य है कि उन दिनों हिन्दू महासभा का कोई स्पष्ट राजनैतिक कार्यक्रम नहीं था और वह मुख्य रूप से हिन्दू संगठन, अछूतोद्धार, शुद्धि जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में ही दिलचस्पी लेती थी। इसी कारण कांग्रेस से उसे थोड़ा भी विरोध नहीं था। यद्यपि संकीर्ण दृष्टि से अनेक राजनैतिक कर्मी लालाजी के हिन्दू महासभा में रुचि लेने से नाराज भी हुए किन्तु उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की और वे अपने कर्तव्यपालन में ही लगे रहे।
जीवन संध्या 1928 में जब अंग्रेजों द्वारा नियुक्त साइमन भारत आया तो देश के नेताओं ने उसका बहिस्कार करने का निर्णय लिया। 30 अक्टूबर, 1928 को कमीशन लाहौर पहुँचा तो जनता के प्रबल प्रतिशोध को देखते हुए सरकार ने धारा 144 लगा दी। लालाजी के नेतृत्व में नगर के हजारों लोग कमीशन के सदस्यों को काले झण्डे दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचे और 'साइमन वापस जाओÓ के नारों से आकाश गुँजा दिया। इस पर पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश मिला। उसी समय अंग्रेज सार्जेंट साण्डर्स ने लालाजी की छाती पर लाठी का प्रहार किया जिससे उन्हें सख्त चोट पहुँची। उसी सायं लाहौर की एक विशाल जनसभा में एकत्रित जनता को सम्बोधित करते हुए नरकेसरी लालाजी ने गर्जना करते हुए कहा-मेरे शरीर पर पडी़ लाठी की प्रत्येक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील का काम करेगी। इस दारुण प्रहात से आहत लालाजी ने अठारह दिन तक विषम ज्वर पीड़ा भोगकर 17 नवम्बर 1928 को परलोक के लिए प्रस्थान किया।
वकालत के क्षेत्र में :- लाला लाजपतराय ने एक मुख्तार (छोटा वकील) के रूप में अपने मूल निवासस्थल जगराँव में ही वकालत आरम्भ कर दी थी; किन्तु यह कस्बा बहुत छोटा था, जहाँ उनके कार्य के बढऩे की अधिक सम्भावना नहीं थी, अत: वे रोहतक चले गये। रोहतक में 1885 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, 1886 में वे हिसार आ गये। एक सफल वकील के रूप में 1892 तक वे यहीं रहे और इसी वर्ष लाहौर आये। तब से लाहौर ही उनकी सार्वजनिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया। लालाजी ने अपने साथियों सहित सामाजिक हित की योजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान किया किन्तु लाहौर आने पर वे आर्यसमाज के अतिरिक्त राजनैतिक आन्दोलन के साथ भी जुड़ गये। 1888 में वे प्रथम बार कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में सम्मिलित हुए जिनकी अध्यक्षता मि0 जार्ज यूल ने की थी। 1906 में वे प0 गोपालकृष्ण गोखले के साथ कांग्रेस के एक शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में इंग्लैड गये। यहाँ से वे अमेरिका चले गये। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएँ की और वहाँ रहकर पश्चिमी देशों के समक्ष भारत की राजनैतिक परिस्थिति की वास्तविकता से वहां के लोगों को परिचित कराया तथा उन्हें स्वाधीनता आन्दोलन की जानकारी दी। लाला लाजपतराय ने अपने सहयोगियों-लोकमान्य तिलक तथा विपिनचन्द्र पाल के साथ मिलकर कांग्रेस में उग्र विचारों का प्रवेश कराया। 1885 में अपनी स्थापना से लेकर लगभग बीस वर्षो तक कांग्रेस ने एक राजभवन संस्था का चरित्र बनाये रखा था। इसके नेतागण वर्ष में एक बार बड़े दिन की छुट्टियों में देश के किसी नगर में एकत्रित होने और विनम्रता पूर्वक शासनों के सूत्रधारों (अंग्रेजी) से सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को अधिकाधिक संख्या में प्रविष्ट युगराज के भारत-आगमन पर उनका स्वागत करने का प्रस्ताव आया तो लालाजी ने उनका डटकर विरोध किया। कांग्रेस के मंच ये यह अपनी किस्म का पहला तेजस्वी भाषण हुआ जिसमें देश की अस्मिता प्रकट हुई थी। 1907 में जब पंजाब के किसानों में अपने अधिकारों को लेकर चेतना उत्पन्न हुई तो सरकार का क्रोध लालाजी तथा सरदार अजीतसिंह (शहीद भगतसिंह के चाचा) पर उमड़ पड़ा और इन दोनों देशभक्त नेताओं को देश से निर्वासित कर उन्हें पड़ोसी देश बर्मा के मांडले नगर में नजरबंद कर दिया, किन्तु देशवासियों द्वारा सरकार के इस दमनपूर्ण कार्य का प्रबल विरोध किये जाने पर सरकार को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा। लालाजी पुन: स्वदेश आये और देशवासियों ने उनका भावभीना स्वागत किया। लालाजी के राजनैतिक जीवन की कहानी अत्यन्त रोमांचक तो है ही, भारतीयों को स्वदेश-हित के लिए बलिदान तथा महान् त्याग करने की प्रेरणा भी देती है।
जन-सेवा के कार्य :- लालाजी केवल राजनैतिक नेता और कार्यकर्ता ही नहीं थे। उन्होंने जन सेवा का भी सच्चा पाठ पढ़ा था। जब 1896 तथा 1899 (इसे राजस्थान में छप्पन का अकाल कहते हैं, क्योंकि यह विक्रम का 1956 का वर्ष था) में उत्तर भारत में भयंकर दुष्काल पड़ा तो लालाजी ने अपने साथी लाला हंसराज के सहयोग से अकालपीडि़त लोगों को सहायता पहुँचाई। जिन अनाथ बच्चों को ईसाई पादरी अपनाने के लिए तैयार थे और अन्तत: जो उनका धर्म-परिवर्तन करने के इरादे रखते थे उन्हें इन मिशनरियों के चुंगुल से बचाकर फीरोजपुर तथा आगरा के आर्य अनाथलायों में भेजा। 1905 में कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में भयंकर भूकम्प आया। उस समय भी लालाजी सेवा-कार्य में जुट गये और डी0ए0वी0 कालेज लाहौर के छात्रों के साथ भूकम्प-पीडि़तों को राहत प्रदान की।
1907-08 में उड़ीसा मध्यप्रदेश तथा संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) से भी भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा और लालाजी को पीडितों की सहायता के लिए आगे आना पड़ा। पुन: राजनैतिक आन्दोलन में 1907 के सूरत के प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपतराय ने अपने सहयोगियों के द्वारा राजनीति में गरम दल की विचारधारा का सूत्रपात कर दिया था और जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गये थे कि केवल प्रस्ताव पास करने और गिड़गिड़ाने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। हम यह देख चुके हैं कि जनभावना को देखते हुए अंग्रेजों को उनके देश-निर्वासन को रद्द करना पड़ा था। वे स्वदेश आये और पुन: स्वाधीनता के संघर्ष में जुट गये। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) के दौरान वे एक प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में पुन: इंग्लैंड गये और देश की आजादी के लिए प्रबल जनमत जागृत किया। वहाँ से वे जापान होते हुए अमेरिका चले गये और स्वाधीनता-प्रेमी अमेरिकावासियों के समक्ष भारत की स्वाधीनता का पथ प्रबलता से प्रस्तुत किया। यहाँ इण्डियन होम रूल लीग की स्थापना की तथा कुछ ग्रन्थ भी लिखे। 20 फरवरी, 1920 को जब वे स्वदेश लौटे तो अमृतसर में जलियावाला बाग काण्ड हो चुका था और सारा राष्ट्र असन्तोष तथा क्षोभ की ज्वाला में जल रहा था। इसी बीच महात्मा गांधी ने सहयोग आन्दोलन आरम्भ किया तो लालाजी पूर्ण तत्परता के साथ इस संघर्ष में जुट गये। 1920 में ही वे कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। उन दिनों सरकारी शिक्षण संस्थानों के बहिस्कार विदेशी वस्त्रों के त्याग, अदालतों का बहिष्कार, शराब के विरुद्ध आन्दोलन, चरखा और खादी का प्रचार जैसे कार्यक्रमों को कांग्रेस ने अपने हाथ में ले रखा था, जिसके कारण जनता में एक नई चेतना का प्रादुर्भाव हो चला था। इसी समय लालाजी को कारावास का दण्ड मिला, किन्तु खराब स्वास्थ्य के कारण वे जल्दी ही रिहा कर दिये गये। 1924 में लालाजी कांग्रेस के अन्तर्गत ही बनी स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गये और केन्द्रीय धारा सभा (सेंटल असेम्बली) के सदस्य चुन लिए गये। जब उनका पं0 मोतीलाल नेहरू से कतिपय राजनैतिक प्रश्नों पर मतभेद हो गया तो उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया और पुन: असेम्बली में पहुँच गये। अन्य विचारशील नेताओं की भाँति लालाजी भी कांग्रेस में दिन-प्रतिदिन बढऩे वाली मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से अप्रसन्नता अनुभव करते थे, इसलिए स्वामी श्रद्धानन्द तथा पं0 मदनमोहन मालवीय के सहयोग से उन्होंने हिन्दू महासभा के कार्य को आगे बढ़ाया। 1925 में उन्हें हिन्दू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। ध्यातव्य है कि उन दिनों हिन्दू महासभा का कोई स्पष्ट राजनैतिक कार्यक्रम नहीं था और वह मुख्य रूप से हिन्दू संगठन, अछूतोद्धार, शुद्धि जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में ही दिलचस्पी लेती थी। इसी कारण कांग्रेस से उसे थोड़ा भी विरोध नहीं था। यद्यपि संकीर्ण दृष्टि से अनेक राजनैतिक कर्मी लालाजी के हिन्दू महासभा में रुचि लेने से नाराज भी हुए किन्तु उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की और वे अपने कर्तव्यपालन में ही लगे रहे।
जीवन संध्या 1928 में जब अंग्रेजों द्वारा नियुक्त साइमन भारत आया तो देश के नेताओं ने उसका बहिस्कार करने का निर्णय लिया। 30 अक्टूबर, 1928 को कमीशन लाहौर पहुँचा तो जनता के प्रबल प्रतिशोध को देखते हुए सरकार ने धारा 144 लगा दी। लालाजी के नेतृत्व में नगर के हजारों लोग कमीशन के सदस्यों को काले झण्डे दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचे और 'साइमन वापस जाओÓ के नारों से आकाश गुँजा दिया। इस पर पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश मिला। उसी समय अंग्रेज सार्जेंट साण्डर्स ने लालाजी की छाती पर लाठी का प्रहार किया जिससे उन्हें सख्त चोट पहुँची। उसी सायं लाहौर की एक विशाल जनसभा में एकत्रित जनता को सम्बोधित करते हुए नरकेसरी लालाजी ने गर्जना करते हुए कहा-मेरे शरीर पर पडी़ लाठी की प्रत्येक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील का काम करेगी। इस दारुण प्रहात से आहत लालाजी ने अठारह दिन तक विषम ज्वर पीड़ा भोगकर 17 नवम्बर 1928 को परलोक के लिए प्रस्थान किया।
महंगाई ने लगाई चहुंओर आग
बढ़ती महंगाई और खाघान्न की समस्या से चहुंओर आग लगी हुई है। इस आग से सबसे प्रभावित है आम नागरिक जिसे दो वक्त की रोटी जुटाना भी अब भारी पड़ रहा है। हालांकि इस तथ्य को झुठलाया नहीं कहा जा सकता की बढ़ती महंगाई के नेपथ्य में सरकारी नीतियों के साथ-साथ संपूर्ण विश्व की गतिविधियां भी कहीं न कहीं कारक के रूप में उपस्थित रहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार सारे मामले को वैश्विक घटनाओं पर थोपकर अपना पल्ला झाड़ ले। विकास का पहिया निरंतर घूमता रहे इसके लिए मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता प्रथम अनिवार्य शर्त है, जिसकी अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। इस समस्या को दो विभिन्न आयामों से देखकर वैश्विक परिपेक्ष्य में सरकार की स्थिति को आंका जा सकता है। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने विश्व में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया था। इस क्रांति की बदौलत न केवल यूरोप विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, अपितु संपूर्ण विश्व ही उसके बनाए रोड मैप का अनुसरण कर प्रगति के पथ पर आगे बढऩे लगा। औद्योगिक क्रांति ने विकास की वो बुनियाद डाली जिस पर आज संपूर्ण संसार की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से टिकी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी औद्योगिक क्रांति की देन माने जा सकते हंै। औद्योगिकीकरण की रफ्तार बनाए रखने के लिए जब कच्चे माल तथा औद्योगिकीकरण के कारण फैक्ट्रियो में बने बहुतायात उत्पादों को खपाने के लिए बस्तियों की आवश्यकता पड़ी तब उपनिवेशवाद का एक नया दौर भी जन्मा था।यह कहना अतिश्योक्ति पूर्ण नहीं है कि औद्योगिकीकरण की वजह से ही हरित एवं श्वेत क्रांति भी अस्तित्व में आ सकीं। बहरहाल, 19वीं शताब्दी की समाप्ति तक वैश्विक मंच और विभिन्न देशों की भौगोलिक सीमाओं में अनेक परिवर्तन आए और वैश्वीकरण की भावना को बढ़ावा मिलने लगा। आ£थक क्षेत्र में सहयोग की बढ़ती आवश्यकता ने सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष:प से एक-दूसरे पर निर्भर बनाकर, स्वयं को सर्वेसर्वा मानने की भावना को रसातल में पहुंचा दिया। यही कारण है कि जब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका पर सबप्राइम संकट छाया तो भारत सहित अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उससे बचने के उपाय ढूंढे जाने शु: हुए। इसी प्रकार खाड़ी देशों से विभिन्न देशों में निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्ररोक्ष:प से प्रभावित करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का बढऩा, महंगाई के बढऩे की दिशा तय करता है, ऐसे में यह कह पाना काफी कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होने वाली हलचलों से कोई देश अब अछूता भी रह सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो महंगाई का मुद्दा एकमात्र सपं्रग सरकार को चिंता का कही विषय नहीं, अपितु इस प्राय: प्रत्येक देश की सरकार अपने-अपने स्तर पर जूझ रही है। वस्तुत: वैश्वीकरण के लाभ और हानि बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की तरह हो चुके हैं जिसके ज्यादा एक्सपोजर से हाय-हाय तो अदाओं पर वाह-वाह करने से लोग नहीं चूकते। कुछ समय पूर्व कैरेबियाई देशों में जो खाधान्न समस्या को लेकर घटनाएं घटित हुई वह इसी प्रभाव का परिणाम मानी जा सकती हैं। इसको लेकर विश्व भर के देश चिंतित होकर अनेक उपाय कर रहे है। आंकड़ों के मुताबिक गत् ढाई दशकों में विश्व का अनाज भंडारण अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच चुका है तथा खाद्यान्न की कीमतें रिकॉर्ड स्तर को पार कर रही हंै। इसको देखते हुए विश्व के कई देशों में अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जा रहे है। तो कहीं आयात पर से प्रतिबंध हटाएं जा रहें हैं। वस्तुत सारी स्थिति ही इस ओर इशारा कर रही हैं कि महंगाई का बढऩा एक मात्र सरकार की असफल नीतियों का परिणाम नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नही लगाया जा सकता कि खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को कम करने में सरकार द्वारा किसी पहल की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी खाद्यान्न की कमी और उनकी कीमतों में वृद्धि को सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखते हंै। चूंकि खाद्यान्न की कीमतों पर अंकुश नहीं लगता, तो इसका सीधा प्रभाव आ£थक विकास और अर्थव्यवस्था पर पडऩा तय है। लेकिन देश में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई इसे समझना भी आवश्यक है। महंगाई बढऩे के दो प्रमुख कारणों सब प्राइम संकट और बढ़ती तेल की कीमतों को निकाल दें तो इसके इत्तर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है जो देश में खाद्यान्न कीमतों की बढ़ोत्तरी के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है और इसका सबसे प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा है। कृषि क्षेत्र के प्रति बरती जाने वाली इसी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग अपने परंपरागत् खेती-बाड़ी के व्यवसाय को छोड़कर अन्य उद्यमों के प्रति आकृष्ट हुआ। चूंकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि ही है, परंतु उसके प्रति बरती गई सरकारी उपेक्षा किसानों का इस दिशा से मोहभंग करने में काफी रही। समय पर सरकारी ऋण न मिलने से परेशान किसान जहां गैर परंपरा गत् उद्यमों की ओर कूच करने लगे वहीं ऋण के बोझ तले दबे किसान एक के बाद एक आत्महत्या करने को बाधित हुई। पिछले कुछ वर्षों का दौर कौन भुला सकता है जब किसानों की आत्महत्या से संबंधित खबरों में समाचार पत्र और टी-वी- चैनल अटे पड़े थे। सहायता के नाम पर नाम मात्र सरकारी धनराशि से किसानों का कितना भला हुआ, यह सहज ही समझा जा सकता है। समय से पूर्व संभावित खाद्यान्न समस्याओं का आंकलन करने में सभी पुरोधा भयंकर चूक कर बैठे। अन्यथा यह कैसे संभव है कि सेंसेक्स की उड़ान पर विकास दर की भविष्यवाणी करने वाले बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप घटती फसल उत्पादकता पर मंथन नहीं कर सके। हां, इस संदर्भ में यह रियायत भले ही ली जा सकती है कि संपूर्ण विश्व में तमाम अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिकों के आंकड़ों से इत्तर यह स्थिति उत्पन्न हुई है।और इसका सबसे प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा है। कृषि क्षेत्र के प्रति बरती जाने वाली इसी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग अपने परंपरागत् खेती-बाड़ी के व्यवसाय को छोड़कर अन्य उद्यमों के प्रति आकृष्ट हुआ। चूंकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि ही है, परंतु उसके प्रति बरती गई सरकारी उपेक्षा किसानों का इस दिशा से मोहभंग करने में काफी रही। समय पर सरकारी ऋण न मिलने से परेशान किसान जहां गैर परंपरा गत् उद्यमों की ओर कूच करने लगे वहीं ऋण के बोझ तले दबे किसान एक के बाद एक आत्महत्या करने को बाधित हुई। पिछले कुछ वर्षों का दौर कौन भुला सकता है जब किसानों की आत्महत्या से संबंधित खबरों में समाचार पत्र और टी-वी- चैनल अटे पड़े थे। सहायता के नाम पर नाम मात्र सरकारी धनराशि से किसानों का कितना भला हुआ, यह सहज ही समझा जा सकता है। समय से पूर्व संभावित खाद्यान्न समस्याओं का आंकलन करने में सभी पुरोधा भयंकर चूक कर बैठे। अन्यथा यह कैसे संभव है कि सेंसेक्स की उड़ान पर विकास दर की भविष्यवाणी करने वाले बढ़ती जनसंख्या के अनरूप घटती फसल उत्पादकता पर मंथन नहीं कर सके। हां, इस संदर्भ में यह रियायत भले ही ली जा सकती है कि संपूर्ण विश्व में तमाम अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिकों के आंकड़ों से इत्तर यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जानकारों का मानना है कि देश में हरित क्रांति के उपरांत एक प्रकार से कृषि क्षेत्र की उपेक्षा प्रारंभ करनी शरू हो गई है। देश में लगातार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलता रहा, जबकि कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत सुविधाओं से जुझने के साथ-साथ अपने विस्तार के लिए तरसते रहें। जिसका परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या के अनुरूप औसतन वार्षिक पैदावार में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी।
सदस्यता लें
संदेश (Atom)