सोमवार, 24 मई 2010
नासूर बना नक्सलवाद
बस्तर के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हाथों सीआरपीएफ के जवानों को बेरहमी से मौत के घाट उतारे जाने के कारण अब सरकार और नक्सली दोनों ही खेमों के बीच लड़ाई के पाले साफ-साफ खिंच गए हैं। इसे नक्सलियों का रणनीतिक प्रतिवाद माना जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस जघन्य हमले के द्वारा अपने बीच फूट पडऩे, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से काडर में घबराहट और दिशाहीनता तथा आदिवासियों द्वारा उनका समर्थन करने से हाथ खींच लेने की खबरों का भी प्रतिहिंसक जवाब देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम द्वारा इस निंदनीय हत्याकाड को सीआरपीएफ की रणनीतिक चूक बताकर पल्ला झाड़ लेने की कोशिश भी नक्सलियों के हौसले बुलंद ही करेगी। नक्सली शायद यह भी जता रहे हैं कि ग्रीन हंट जैसे अभियान चलाकर सरकार उनके ही गढ़ में उन पर हावी नहीं हो सकती, लेकिन नक्सली इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार करते हुए यह भूल गए कि सीआरपीएफ के हलाक हुए जवान भी उसी दबे-कुचले वर्ग के हैं, जिसके हितों की रक्षा के लिए वह अपनी हिंसा और हथियार की राजनीति को सही ठहराते हैं। लोकतंत्र के लिए यह बहुत बुरी खबर है, लेकिन सरकार को यह बात समझ में नहीं आ रही कि नक्सली तो सशस्त्र क्राति के घोषित हामी हैं [हालाकि इससे वह सही नहीं हो जाते], पर गाधी के सिद्धातों पर चलने वाली सरकार को क्या हो गया है। आदिवासी कल्याण और जनजातियों की रक्षा का दम भरने वाली सरकार की यह कैसी सोची-समझी रणनीति है और ऐसे कौन से उनके सलाहकार हैं, जो आदिवासियों और उन इलाकों की तासीर ही नहीं जानते-समझते। वे कैसे नहीं जानते कि गोली चाहे जिस तरफ से चले, गिरेगा सिर्फ आदिवासी। सिर्फ उसी का खून बहेगा। नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में लड़ाई आसान नहीं है। वहा जंगल वार के जानकार चाहिए, इसीलिए नागालैंड का विशेष सशस्त्र बल और र्अ्धसैनिक दस्ते इन इलाकों में तैनात है। सोचिए, क्या नगा आदिवासी नहीं हैं? मिजो बल में किनकी बहुतायत होगी? नक्सलियों का साथ देने वाले आदिवासी ही हैं। ऐसे में कितना आदिवासी खून बहेगा और ऐसे खून-खराबे के बाद क्या आदिवासी कभी मुख्यधारा से जुड़ पाएगा। देश में करीब आठ करोड़ आदिवासी हैं यानी देश की कुल आबादी का लगभग आठ प्रतिशत। जहा आज मुठभेड़ हुई है, वह अति नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक संवेदनशील इलाका है। राज्य के कुल भूभाग में से 44 फीसदी वनक्षेत्र है और उसी में आदिवासी बसाहट है और शायद देश ही नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी इलाका है। बस्तर के इस आदिवासी अंचल में आज भी ऐस घने जंगल हैं, जहा सूरज की रोशनी धरती को नहीं छू पाती। इलाके के पुराने बाशिदों को भले ही जंगलों की कटाई पर अफसोस हो, लेकिन बाहरी लोगों के लिए आज भी बस्तर घने जंगलों और डरावने आदिवासियों का रहस्य-रोमाच भरा इलाका है। बस्तर के ये बचे-खुचे नायाब जंगल, जिन्हें आदिवासी देवतुल्य और मा दंतेश्वरी की कृपा मानते हैं, दुनिया को उनके इन्हीं आदि सनातन निवासियों की देन हैं। इन्हीं के प्रयासों से यह बचे हुए हैं। जब से जंगल कानून अस्तित्व में आए हैं आदिवासियों की खेती-बाड़ी, महुआ, टोरा जैसी जरूरत भर की वनोपज से लेकर झाडिय़ों की ओट में हाजत तक के नैसर्गिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहे हैं। अपने पोसे जंगलों में घुसने तक के लिए वह वन विभाग के अदने कर्मचारियों के रहमोकरम का मोहताज है। और जंगल के कर्मचारी तो ऐसे अधिकार पाकर जैसे मतवाले हो गए हैं। आदिवासियों पर मनमाने आरोप लगाकर उन्हें सताना और उनसे उगाही करना जैसे उनका धर्म बन गया है। पुलिस का सलूक इन बेजुबान आदिवासियों से और बुरा है। आदिवासी फरियाद करें तो बोली की दिक्कत। कहीं उन्हें समझने और उनका हमदर्द बनने की ललक ही नहीं। वैसे तो इन कम कपड़ों वाले सावले आदिवासियों के प्रति जबरदस्त हिकारत, पर उनकी युवा बेटियों का दैहिक शोषण करते समय जरा भी झिझक नहीं। जब रखवाला ही आपकी बात न समझे तो किससे फरियाद करें ये आदिवासी। यह प्रशासनिक हिकारत और शोषण ही है, जिसने आदिवासी अंचलों में नक्सलवाद को पैठाया और कभी भिंडरावाले से हलकान काग्रेस अब उसी अंदाज में नक्सलवाद को सबसे खतरनाक आतंकवाद बताकर इसके सफाये के लिए मुनादी पीट रही है। वैसे ताच्जुब यह है कि जिस नक्सलवाद को काग्रेस हाल तक सामाजिक-आर्थिक समस्या बताकर बातचीत करने की बात कहती थी, वह चंद महीनों पहले रातों-रात आतंकवाद हो गया। काग्रेस के अजीत जोगी से लेकर न जाने कितने नेताओं ने लगातार ऐसे बयान दिए। दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महिला पत्रकारों से मुलाकात के समय खुद इस लेखक से नक्सलवाद को सामाजिक-आर्थिक समस्या कहा था। देश में आधी सदी से ऊपर राज कर चुके इतने बड़े राजनीतिक दल के रुख में अचानक इस बदलाव का कारण संदिग्ध ही है। वैसे भी नक्सल प्रभावित इलाकों में औद्योगिकरण की जैसी सुगबुगाहट है, उससे यह भी शक होता है कि कहीं हम अपने आदिवासियों से वैसा व्यवहार तो नहीं करने जा रहे हैं, जैसा कभी अमेरिका ने अपने ऐबोरिजिनिस यानी वहा के आदिवासियों के साथ किया था। अमेरिका में औद्योगिकरण के इतिहास का नजारा आज के भारत जैसा ही है। फर्क यह है कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी हैं। वे आर्यो की तरह भारत में बाहर से नहीं आए थे, बल्कि द्रविड़ों की तरह भारत के मूल निवासी है। इनका दुर्भाग्य यह है कि प्रकृति ने देश के इन सबसे गरीब लोगों की धरती में ही सारा वैभव उड़ेल दिया है। यही प्राकृतिक वैभव इनकी जान का जोखिम बन गया है। टाटा, एस्सार और वेदात सभी को वनाच्छादित इन इलाकों में कारखाने लगाने हैं। इनके खनिज का दोहन करना है। चाहे छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा या झारखड, इन सभी का प्राकृतिक वैभव व्यापारियों को भरमा रहा है। वे सत्ता के गलियारों में पैरवी कर रहे हैं और नेता उनके पैरोकार बन गए हैं। यह कवायद जबसे शुरू हुई है, आदिवासी बेचैन हैं। बस्तर में एक कहावत है कि मैना बोलती है और आदिवासी बेजुबान है। उसकी जुबान कोई समझ नहीं पा रहा है। नक्सलियों ने उसकी बात समझनी शुरू की तो उनके हमदर्द बन गए। जबकि नेता हमेशा उनसे नमक के बदले मोटी फूल झाडू खरीदकर एक की दस झाडू बनाकर बेचने वाले व्यापारी का साथ देते रहे, तेंदू पत्ता की खरीदी में दलाली खाते रहे और नक्सलियों ने आदिवासियों को सही कीमत दिलाई तो उनकी दुकानें बंद हो गई। नक्सल-आदिवासियों में अंतरंगता बढ़ी तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। नक्सल प्रभावित राज्यों का सच यही है कि ज्यादातर नेता इनकी मदद लेकर ही चुनाव लड़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने नक्सलियों पर कार्रवाई का यों ही विरोध नहीं किया था। इन इलाकों की हकीकत यही है कि जहा सरकार नाकाम रही, वहा नक्सलियों ने काम किए। आदिवासियों में उन्होंने वह आत्मविश्वास जगाया, जो सरकार और नेताओं को जगाना चाहिए था। सलवाजुडूम के सिरमौर महेंद्र कर्मा भी कभी नक्सलियों से निकटता के लिए जाने जाते थे। वे अब नक्सलियों के कट्टर दुश्मन हैं और उनकी हिटलिस्ट में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नक्सलियों ने अपने प्रभाव वाले इलाकों में बेहिसाब ऐसे काम किए हैं, जिनसे सरकार चाहे तो सबक ले सकती है, लेकिन अब ग्रीन हंट से बौखलाकर इतना बड़ा नरसंहार करके वह अपने किए पर ही पानी फेर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा का पूरा अभियान जिन महिलाओं को स्कूल की चौखट पर नहीं ला पाया, वे अब नक्सलियों के प्रयास से पढ़ रही हैं। पुरुषों के लिए भी घरेलू काम-काज में उनकी भागीदारी पर कक्षा होती है। इस सबके बावजूद ऐसी सिरफिरी हिंसा का कोई तुक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें चुनौती दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की निर्वाचित सरकार ने दी है, जो अपने ही नागरिकों को समझा-बुझाकर कोई राजनैतिक रास्ता निकालने के बजाय उन्हें ताकत के बूते खत्म करने पर उतारू है। यह भी सच है कि सरकार के आगे लंबे समय तक टिक पाना नक्सलियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के पास न जान गंवाने वाले जवानों की कमी है और न ही अस्त्र-शस्त्रों की, मगर नक्सलियों और सरकार अहिंसा और बातचीत की गाधीवादी परंपरा का पालन करेगी या भारत में भी अमेरिका के इतिहास को दोहराए जाने का इंतजार करेगी।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)

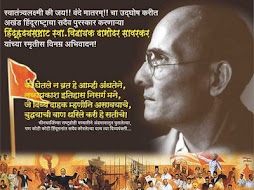














कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें